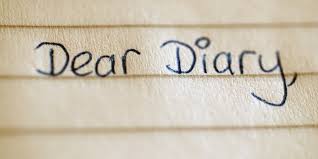|
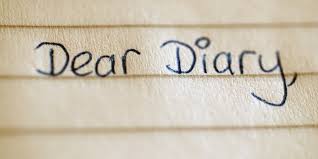
पुस्तक अंश
रसूल हमाजातोव का दाग़िस्तान

( रसूल हमाजतोव की यह
आत्मकथात्म पुस्तक एक जीवन-डायरी का अहसास देती है, इसका सौंदर्य इसके
प्राकृतिक विवरणों में है। अपने पाठकों के लिए एक रोचक अंश)
मेरी
पुस्तक,
बहुत सालों तक तुम
मेरी आत्मा में जीती रही हो! तुम उस औरत,
दिल की उस
रानी के समान हो,
जिसे उसका प्रेमी
दूर से देखा करता है,
जिसके सपने देखता
है,
मगर जिसे छूने का
उसे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि वह बिल्कुल
नजदीक ही खड़ी रही है - बस,
हाथ बढ़ाने की ही
जरूरत थी,
मगर मेरी हिम्मत न
हुई,
मैं झेंप गया,
मेरे मुँह
पर लाली दौड़ गई और मैं दूर हट गया।
पर अब यह सब खत्म
हो चुका है। मैंने साहसपूर्वक उसके पास जाने और उसका हाथ अपने हाथ में लेने
का निर्णय कर लिया है। झेंपू प्रेमी की जगह मैं साहसी और अनुभवी मर्द बनना
चाहता हूँ। मैं घोड़े पर सवार होता हूँ,
तीन बार
चाबुक सटकारता हूँ - जो भी होना हो,
सो हो!
फिर भी मैं अपने
कड़वे देसी तंबाकू को कागज पर डालता हूँ,
इतमीनान से
सिगरेट लपेटता हूँ। अगर सिगरेट लपेटने में ही इतना मजा है,
तो कश लगाने
में कितना मजा होगा!
मेरी पुस्तक,
तुम्हें
शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि कैसे तुमने मेरी आत्मा में
रूप धारण किया। कैसे मैंने तुम्हारा नाम चुना। किसलिए मैं तुम्हें लिखना
चाहता हूँ। जीवन में मेरे क्या उद्देश्य-लक्ष्य हैं।
मेहमान को मैं
रसोईघर में जाने देता हूँ,
जहाँ अभी भेड़ का
धड़ साफ किया जा रहा है और अभी सीख-कबाब की नहीं,
लहू और गर्म
मांस की गंध आ रही है।
दोस्तों को मैं
अपने पावन कार्य-कक्ष में ले जाता हूँ,
जहाँ मेरी
पांडुलिपियाँ रखी हैं,
और मैं उन्हें
उनको पढ़ने की इजाजत देता हूँ।
मेरे पिता जी चाहे
यह कहा करते थे कि जो कोई पराई पांडुलिपियाँ पढ़ता है,
वह दूसरों
की जेब में हाथ डालनेवाले के समान है।
पिता जी यह भी कहा
करते थे कि भूमिका थियेटर में तुम्हारे सामने बैठे चौड़े-चकले कंधों और
साथ ही बड़ी टोपीवाले आदमी की याद दिलाती है। अगर वह टिककर बैठा रहे,
दाएँ-बाएँ न
हिले,
तो भी गनीमत समझिए।
दर्शक के नाते ऐसे आदमी से मुझे बड़ी असुविधा और आखिर झल्लाहट होने लगती
है।
नोटबुक से। मुझ
मास्को या रूस के दूसरे शहरों में अक्सर कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेना
पड़ता है। हॉल में बैठे लोग अवार भाषा नहीं जानते होते। शुरू में अशुद्ध
उच्चारण के साथ में जैसे-तैसे रूसी भाषा में अपने बार में कुछ बताता हूँ।
इसके बाद मेरे दोस्त,
रूसी कवि,
मेरी
कविताओं का अनुवाद सुनाते हैं। मगर उनके शुरू करने के पहले आमतौर पर मुझसे
मेरी मातृभाषा में एक कविता सुनाने का अनुरोध किया जाता है,
'हम अवार
भाषा और कविता के संगीत का रस लेना चाहते हैं।'
मैं सुनाता
हूँ,
मगर मेरा कविता-पाठ
गाना शुरू होने के पहले पंदूर की झनझनाहट के सिवा और कुछ नहीं होता।
तो क्या मेरी
किताब की भूमिका भी ऐसी ही नहीं है ?
नोटबुक से । मैं जब
विद्यार्थी था,
तो जाड़े का ओवरकोट
खरीदने के लिए पिता जी ने मुझे पैसे भेजे। पैसे तो मैंने खर्च कर डाले और
ओवरकोट नहीं खरीदा। जाड़े की छुट्टियों में वही हल्का-सा ओवरकोट पहने हुए,
जिसे
गर्मियों में पहनकर मैं मास्को पढ़ने आया था,
दागिस्तान
जाना पड़ा।
घर पर पिता जी के
सामने मैं अपनी सफाई पेश करने लगा,
तुरत-फुरत
एक से एक बेतुका और बेसिर-पैर का क्रिस्सा गढ़कर सुनाने लगा। जब मैं अपने
ही ताने-बाने में पूरी तरह उलझ गया,
तो पिता जी
ने मुझे टोकते हुए कहा -
'रुको,
रसूल। मैं
तुमसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ।'
'पूछिए।'
'ओवरकोट
खरीदा?'
'नहीं।'
'पैसे
खर्च कर दिए!'
'हाँ।'
'बस,
अब सारी बात
साफ हो गई। अगर दो लफ्जों में ही मामले का निचोड़ निकल सकता है,
तो किसलिए
तुमने इतने बेकार शब्द कहे,
इतनी लंबी-चौड़ी
भूमिका बाँधी?'
मेरे पिता जी ने
मुझे ऐसी शिक्षा दी थी।
फिर भी बच्चा पैदा
होते ही नहीं बोलने लगता। शब्द कहने से पहले वह अपनी तुतली भाषा में कुछ
ऐसा बोलता है,
जो किसी के पल्ले
नहीं पड़ता। ऐसा भी होता है कि जब वह दर्द से रोता-चिल्लाता है,
तो माँ के
लिए भी यह जानना मुश्किल हो जाता है कि उसे किस जगह पर दर्द हो रहा है।
क्या कवि की
आत्मा बच्चे की आत्मा जैसी नहीं होती
?
पिता जी कहा करते
थे कि लोग जब पहाड़ों से भेड़ों के रेवड़ के आने का इंतजार करते हैं,
तो सबसे
पहले उन्हें हमेशा आगे-आगे आनेवाले बकरे के सींग दिखाई देते हैं,
फिर पूरा
बकरा नजर आता है और इसके बाद ही वे रेवड़ को देख पाते हैं।
लोग जब शादी के या
मातमी जुलूस की राह देखते हैं,
तो पहले तो
उन्हें हरकारा दिखाई देता है।
गाँव के लोग जब
हरकारे के इंतजार में होते हैं,
तो पहले तो
उन्हें धूल का बादल,
फिर घोड़ा और उसके
बाद ही घुड़सवार नजर आता है।
लोग जब शिकारी के
लौटने की प्रतीक्षा में होते हैं,
तो पहले तो
उन्हें उसका कुत्ता ही दिखाई देता है।
वसंत के दिनों में
वसंत का एक पक्षी किसी गाँव में उड़ता हुआ आया। लगा सोचने कि बैठकर आराम
करे। एक पहाड़ी घर की चौड़ी,
समतल और साफ छत पर
नजर पड़ी। छत पर उसे समतल करने के लिए पत्थर का रोलर है। पक्षी आसमान से
नीचे उतरा और रोलर पर आराम करने बैठ गया। चुस्त पहाड़िन पक्षी को पकड़कर घर
में ले गई। पक्षी ने देखा कि घर के सभी लोग उसके साथ अच्छे ढंग से पेश आते
हैं और इसलिए वहीं रहने लगा। उसने धुएँ से काले हुए पुराने शहतीर पर ठोंके
गए नाल में अपना घोंसला बना लिया।
क्या मेरी किताब
के बारे में भी यही बात नहीं है?
कितनी ही बार मैंने
अपने काव्य-गगन से नीचे,
गद्य के समतल मैदान
पर यह ढूँढ़ते हुए नजर डाली कि कहाँ बैठकर आराम करूँ...
नहीं,
इस सिलसिले
में उस हवाई जहाज से तुलना करना ज्यादा ठीक होगा,
जिसे हवाई
अड्डे पर उतरना है। लीजिए,
मैं चक्कर काटता
हूँ ताकि नीचे उतरने लगूँ। मगर बुरे मौसम के कारण हवाई अड्डेवाले मुझे ऐसा
करने की इजाजत नहीं देते। बहुत बड़ा चक्कर काटने के बजाय मैं फिर से सीधी
उड़ान भरता हुआ आगे उड़ने लगता हूँ और वांछित पृथ्वी फिर नीचे ही रह जाती
है... अनेक बार ऐसा ही हो चुका है।
तो मैंने सोचा,
इसका तो यही
मतलब निकलता है कि कंकरीट का मजबूत आधार मेरी किस्मत में नहीं लिखा है।
इसका तो यही अर्थ है कि मेरे पैरों को धरती पर अविराम चलते ही जाना होगा,
मेरी आँखों
को निरंतर पृथ्वी की नई जगहों को खोजते रहना होगा,
मेरे हृदय
को लगातार नए गीत रचने होंगे।
जिस तरह कोई हलवाहा
आसमान में तैरते दूधिया बादल या तिकोन बनाकर उड़े जाते सारसों को देखते हुए
अपनी सुध-बुध भूल जाता है,
मगर कुछ ही क्षण
बाद इस जादू से मुक्त हो अधिक उत्साह के साथ हल चलाने लगता है,
उसी तरह मैं
अधूरी छोड़ी गई अपनी लंबी कविता की ओर लौटा हूँ।
हाँ,
मेरी कविता,
मैं
अंतरिक्ष से उसकी चाहे कितनी भी तुलना क्यों न करूँ,
मेरे लिए वह
मेरी ठोस जमीन थी,
मेरा खेत थी,
मेरा गाढ़ा
पसीना थी। अब तक गद्य को मैंने बिल्कुल ही नहीं लिखा था।
तो एक दिन मुझे एक
पैकेट मिला। पैकेट में उस पत्रिका के संपादक का पत्र था,
जिसका मैं
बहुत आदर करता हूँ। वैसे,
आदर तो मैं संपादक
का भी बहुत करता हूँ। हाँ,
संपादक ने भी अपना
पत्र 'आदरणीय
रसूल'
शब्दों के साथ
शुरू किया था। कुल मिलाकर,
गहरी पारस्परिक
आदर भावना सामने आई।
पत्र को जब मैंने
खोला,
तो वह मुझे भैंस की
उस खाल का-सा प्रतीत हुआ,
जिसे पहाड़ी लोग
अच्छी तरह सुखाने के लिए अपने घर की सपाट छत पर फैला देते हैं। अच्छी तरह
सूख चुकी भैंस की खाल को घर में ले जाने के लिए जब तह लगाई जाती है,
तो वह जितनी
आवाज करती है,
इसी तरह उस पत्र को
पढ़ते समय उसके कागजों ने भी कुछ कम सरसराहट नहीं की। सिर्फ खाल की तेज नाक
में खुजली-सी पैदा करनेवाली गंध नहीं थी। पत्र से किसी भी तरह की गंध नहीं
आ रही थी।
खैर,
तो संपादक
ने यह लिखा था, 'हमारे
संपादकमंडल ने अपनी पत्रिका के अगले कुछ अंकों में दागिस्तान की
उपलब्धियों,
शुभ कार्यों और
सामान्य श्रम दिवसों के बारे में सामग्री छापने का निर्णय किया है। यह आम
मेहनतकशों,
उनके साहसपूर्ण
कार्यों,
उनकी
आशाओं-आकांक्षाओं की कहानी होनी चाहिए। यह कहानी होनी चाहिए तुम्हारे
पहाड़ी प्रदेश के उज्ज्वल 'भविष्य'
उसकी सदियों
पुरानी परंपराओं की,
मगर मुख्यतः यह
कहानी होनी चाहिए उसके भव्य 'वर्तमान'
की। हमने तय
किया है कि ऐसी कहानी तुम ही सबसे बेहतर लिख सकते हो। इसके लिए विधा तुम
अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हो - कहानी,
लेख,
रेखाचित्र,
कुछ लघु
शब्द चित्र - किसी भी रूप में लिख सकते हो। सामग्री
9-10
टाइप पृष्ठों की ही और 20-25
दिनों में पहुँच जाए। हमें तुम्हारे सहयोग की पूरी आशा है और तुम्हें
पहले से ही धन्यवाद देते हैं...'
कभी वह जमाना था कि
लड़की की शादी करते हुए उसकी सहमति नहीं ली जाती थी। बस,
शादी कर दी
जाती थी। या जैसे कि आजकल कहा जाता है,
शादी का
तथ्य उसके सामने रख दिया जाता था। मगर उन वक्तों में भी हमारे पहाड़ों
में बेटे की रजामंदी के बिना कोई उसकी शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकता
था। सुनने में आया है कि किसी हीदातलीवासी ने एक बार ऐसा किया था। मगर मेरा
सम्मानित संपादक क्या हीदातली गाँव का रहनेवाला है?
मेरे लिए
उसने ही सब कुछ तय कर लिया... मगर क्या मैंने नौ पृष्ठों और बाईस दिन की
अवधि में अपने दागिस्तान के बारे में बताने का निर्णय किया है?
अपने लिए अपमानजनक
इस पत्र को मैंने झल्लाहट में कहीं दूर फेंक दिया। मगर कुछ दिन बाद मेरे
टेलीफोन की घंटी ऐसे लगातार बजने लगी,
मानो वह
टेलीफोन की घंटी न होकर अंडा देनेवाली मुर्गी हो। जाहिर है कि पत्रिका के
संपादकीय कार्यालय का ही यह टेलीफोन था।
'सलाम,
रसूल! हमारा
खत मिला?'
'हाँ।'
'सामग्री
का क्या हुआ?'
'सामग्री...
मैं काम-काज में उलझा रहा... फुरसत नहीं मिली।'
'यह
तुम क्या कह रहे हो,
रसूल! भला ऐसा कैसे
हो सकता है! हमारी पत्रिका की तो लगभग दस लाख प्रतियाँ छपती हैं। विदेशों
में भी उसके पाठक हैं। पर यदि तुम सचमुच ही बहुत व्यस्त हो,
तो हम कोई
आदमी तुम्हारे पास भेज देते हैं। तुम अपने कुछ विचार और तफसीलें उसे बता
देना,
बाकी वह सब कुछ खुद
ही कर लेगा। तुम उसे पढ़कर,
ठीक-ठाक करके उस पर
अपने हस्ताक्षर कर देना। हमारे लिए तो मुख्य चीज तुम्हारा नाम है।'
'मेहमान
को देखकर जो नाखुश हो,
उसकी सारी हड्डियाँ
टूट जाएँ। अगर कोई मेहमान के आने पर रोनी सूरत बनाए या नाक-भौंह चढ़ाए,
तो उसके घर
में न तो बड़े ही रहें,
जो अक्लमंद नसीहत
दे सकें और न छोटे ही रहें,
जो उन नसीहतों को
सुन सकें! ऐसा है मेहमानों के बारे में हम पहाड़ी लोगों का दृष्टिकोण। मगर
खुदा के लिए कोई मददगार नहीं भेजिएगा। अपना साज मैं उसके बिना ही सुर में
कर लूँगा। अपनी गागर का हत्था भी मैं खुद ही तैयार कर लूँगा। अगर पीठ पर
खुजली होगी तो खुद मुझसे बेहतर तो कोई उसे नहीं खुजा सकेगा।'
बस,
यहाँ हमारी
बातचीत का अंत हो गया। वा सलाम,
वा कलाम!
मैंने एक महीने की छुट्टी ली और अपने जन्म-गाँव त्सादा चला गया।
त्सादा... सत्तर
गर्म चूल्हे। निर्मल और ऊँचे आकाश में सत्तर चिमनियों से नीला धुआँ उठा
करता है। काली धरती पर सफेद पहाड़ी घर हैं। गाँव,
सफेद घरों
के सामने हरे,
समतल मैदान हैं।
गाँव के पीछे चट्टानें ऊपर को उठती चली गई हैं। हमारे गाँव के ऊपर भूरी
चट्टानों का ऐसा जमघट है मानो बालक नीचे,
शादीवाले
अहाते में झाँकने के लिए समतल छत पर इकट्ठे हुए हों।
त्सादा
गाँव में आने पर मुझे पिता जी का वह खत याद हो आया,
जो पहली बार
मास्को देखने पर उन्होंने हमें लिखा था। यह समझ पाना मुश्किल था कि पिता
जी ने अपने खत में किस जगह पर मजाक किया है और कहाँ संजीदगी से बात लिखी
है। मास्को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई थी -
'ऐसा
लगता है कि यहाँ मास्को में खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती,
क्योंकि
मुझे यहाँ अपने घरों की दीवारों पर उपले पाथनेवाली औरतें नजर नहीं आतीं,
घरों की
छतों के ऊपर अबूतालिब की बड़ी टो पी
जैसा धुआँ नहीं दिखाई देता। छत को समतल करने के लिए रोलर भी नजर नहीं आते।
मास्कोवासी अपनी छतों पर घास सुखाते हों,
ऐसा भी नहीं
लगता। पर यदि घास नहीं सुखाते,
तो अपनी
गायों को क्या खिलाते हैं?
सूखी टहनियों या
घास का गट्ठा उठाए एक भी औरत कहीं नजर नहीं आई। न तो कभी जुरने की झनक और न
खंजड़ी की ढमक ही सुनाई दी है। ऐसा लग सकता है मानो जवान लोग यहाँ शादियाँ
ही नहीं करते और ब्याह का धूम-धड़ाका ही नहीं होता। इस अजीब शहर की
गलियों-सड़कों पर मैंने कितने भी चक्कर क्यों न लगाए,
कभी एक बार
भी कोई भेड़ नजर नहीं आई। तो सवाल पैदा होता है कि जब कोई मेहमान आता है,
तो
मास्कोवाले क्या जिबह करते हैं! अगर भेड़ को जिबह करके नहीं,
तो
यार-दोस्त के आने पर वे कैसे उसकी खातिरदारी करते हैं! नहीं,
ऐसी जिंदगी
मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपने त्सादा गाँव में ही रहना चाहता हूँ,
जहाँ बीवी
से यह कहकर कि वह कुछ ज्यादा लहसुन डालकर खीनकाल बनाए,
उन्हें जी
भरकर खाया जा सकता है...' पी
जैसा धुआँ नहीं दिखाई देता। छत को समतल करने के लिए रोलर भी नजर नहीं आते।
मास्कोवासी अपनी छतों पर घास सुखाते हों,
ऐसा भी नहीं
लगता। पर यदि घास नहीं सुखाते,
तो अपनी
गायों को क्या खिलाते हैं?
सूखी टहनियों या
घास का गट्ठा उठाए एक भी औरत कहीं नजर नहीं आई। न तो कभी जुरने की झनक और न
खंजड़ी की ढमक ही सुनाई दी है। ऐसा लग सकता है मानो जवान लोग यहाँ शादियाँ
ही नहीं करते और ब्याह का धूम-धड़ाका ही नहीं होता। इस अजीब शहर की
गलियों-सड़कों पर मैंने कितने भी चक्कर क्यों न लगाए,
कभी एक बार
भी कोई भेड़ नजर नहीं आई। तो सवाल पैदा होता है कि जब कोई मेहमान आता है,
तो
मास्कोवाले क्या जिबह करते हैं! अगर भेड़ को जिबह करके नहीं,
तो
यार-दोस्त के आने पर वे कैसे उसकी खातिरदारी करते हैं! नहीं,
ऐसी जिंदगी
मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपने त्सादा गाँव में ही रहना चाहता हूँ,
जहाँ बीवी
से यह कहकर कि वह कुछ ज्यादा लहसुन डालकर खीनकाल बनाए,
उन्हें जी
भरकर खाया जा सकता है...'
मेरे पिता जी ने
अपने जन्म-गाँव के मुकाबले में मास्को में और भी बहुत-सी खामियाँ खोज
निकालीं। जाहिर है कि जब उन्होंने इस बात की हैरानी जाहिर की थी कि
मास्को के घरों पर उपले नहीं पाथे हुए थे,
तो मजाक
किया था,
मगर जब बड़े शहर के
मुकाबले में अपने जन्म गाँव को तरजीह दी थी,
तो उसमें
मजाक नहीं था। वे अपने त्सादा को प्यार करते थे और उसके मुकाबले में
दुनिया की सभी राजधानियों को ठुकरा देते।
प्यारे त्सादा!
तो लो उस बहुत बड़ी दुनिया से मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ,
जिसमें मेरे
पिता जी को ही इतनी ज्यादा खामियाँ नजर आई थीं। मैं घूम आया हूँ इस दुनिया
में और बहुत-से अजूबे देखे हैं मैंने। इतनी ज्यादा खूबसूरती देखने को मिली
कि आँखें यही तय न कर पाईं कि वे कहाँ टिकें। एक सुंदर मंदिर-मसजिद से मेरी
नजर दूसरे मंदिर-मसजिद की तरफ भागती रही,
एक खूबसूरत
चेहरे से दूसरे खूबसूरत चेहरे की तरफ खिंचती रही। मगर मैं जानता था कि जो
कुछ इस वक्त देख रहा हूँ,
वह चाहे कितना ही
खूबसूरत क्यों न हो,
कल मुझे उससे भी
ज्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी... दुनिया का तो कोई ओर-छोर ही न ठहरा।
भारत के पगोडा,
मिस्र के
पिरामिड,
इटली के बाजीलिक
मुझे माफ करें,
अमरीका के राजमार्ग,
पेरिस के
बुलवार,
इंग्लैंड के पार्क
और स्विटजरलैंड के पहाड़ मुझे क्षमा करें,
पोलैंड,
जापान और
रोम की औरतों से मैं माफी चाहता हूँ - मैं तुम सब पर मुग्ध हुआ,
मगर मेरा
दिल चैन से धड़कता रहा। अगर उसकी धड़कन बढ़ी भी,
तो इतनी
नहीं कि गला सूख जाता और सिर चकराने लगता।
पर अब जब मैंने
चट्टान के दामन में बसे हुए इन सत्तर घरों को फिर से देखा है,
तो मेरा दिल
ऐसे क्यों उछल रहा है कि पसलियों में दर्द होने लगा है,
आँखों के
सामने अँधेरा छा गया है और सिर ऐसे चकराने लगा है मानो मैं बीमार या नशे
में धुत्त होऊँ!
क्या
दागिस्तान का छोटा-सा गाँव वेनिस,
काहिरा या
कलकत्ते से बढ़कर है?
क्या लकड़ियों का
गट्ठा उठाए पगडंडी पर जानेवाली अवार औरत स्केंडिनोविया की ऊँचे कद और
सुनहरे बालोंवाली सुंदरी से बढ़कर है?
-रसूल हमज़ातोव
Top
|