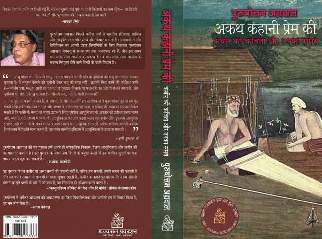|
|

जो कलि नाम कबीर न
होते...’ जिज्ञासाएं और समस्याएं
-
डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल
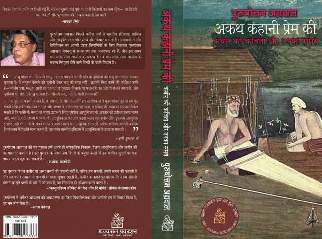
1.बेचैनी, जिज्ञासा और यात्रा: कबीर से मेरा नाता.
2. स्मृति, खोज और देशभाषा के स्रोतः किस्सा
राजू गाइड का.
3. आधुनिकताः देशज बनाम औपनिवेशिक.
4.मानवीय चैतन्य का साझा सपना.
5. ‘जन कबीर का सिखरि घर’: फैंटेसी, यूटोपिया और
धर्मेतर अध्यात्म.
1.बेचैनी, जिज्ञासा और
यात्रा: कबीर से मेरा नाता
कबीर के अध्ययन की समस्याएं भक्ति-संवेदना के, भारतीय
इतिहास के अध्ययन की समस्याएं भी हैं। इस अध्याय में इन समस्याओं की ओर
तथा उन पर विचार करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत किए गए
हैं। यहीं आपको इस पुस्तक में उठाए गए प्रश्नों और खोजे गए उत्तरों का
शुरुआती परिचय भी मिल जाएगा।
भारत, बल्कि किसी भी गैर-यूरोपीय समाज के अतीत और
वर्तमान को समझने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है- चेतना का उपनिवेशीकरण।
कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी राज की स्थापना के पहले का भारत धरा पर
स्वर्ग समान था। हमारी हर समस्या विदेशियों की देन है। दूसरे शब्दों में,
अपनी समस्याएं हल तो हम क्या करेंगे, इतनी भी सामर्थ्य परमात्मा ने
भारतीयों को नहीं दी है कि अपने लिए कुछ समस्याएं खुद भी पैदा कर सकें।
दूसरी ओर, कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी राज आया
तो मुक्ति आई, प्रगति आई, आधुनिकता आई, वरना तो भारतीय समाज तो जैसे बर्फ
में जमा हुआ था। अंग्रेजी राज के पहले के भारतीय जन-जीवन में,
अत्याचारों और तर्कविहीन परंपराओं के अंधानुगमन के सिवाय, था क्या?
परस्पर विरोधी दिखने वाले ये मूल्यांकन असल में एक
ही जमीन पर खड़े हैं। वह जमीन है— औपनिवेशिक ज्ञानकांड की जमीन। इस जमीन पर
खडे़ होकर यह नहीं दिखता कि औपनिवेशिक ज्ञानकांड भारतीय समाज का
‘वस्तुनिष्ठ अध्ययन’ नहीं कर रहा था। वह समाज में ,उसके परंपरा-बोध और
दैनंदिन जीवन में मूलगामी और दूरगामी हस्तक्षेप, बल्कि तोड़-फोड़ कर
रहा था। इस हस्तक्षेप में अंतर्निहित थी—यूरोपीय आधुनिकता की अहम्मन्यता और
साम्राज्यवाद की क्रूरता।
इस हस्तक्षेप के इतिहास और परिणामों का बोध प्राप्त
किए बिना, कबीर के समय के भारत का प्रामाणिक बोध प्राप्त करना असंभव है।
ऐसा प्रामाणिक बोध प्राप्त करने की पहली शर्त्त हैः देशभाषा के स्रोतों से
गहराई के साथ गुजरना और समाज के दैनंदिन व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना।
कबीर को ‘पढ़ने’ के लिए, एक तरफ देशज मनीषा को,और
दूसरी तरफ औपनिवेशिक हस्तक्षेप को ‘पढ़ना’ अनिवार्य है—यह अहसास मुझे भगवान
के दर्शन की तरह एकाएक नहीं, निरंतर चलती आ रही जिज्ञासा-यात्रा के दौरान
ही प्राप्त हुआ है। कबीर से मेरा क्या नाता है—यह भी इसी यात्रा में समझ
आया।
नवलदास से मिलना इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था।
दस बरस बीत चले। सन निन्यानवे के दिसंबर में, बनारस
में नवलदास जी से भेंट हुई थी। जाति के कुरमी, ये बुजुर्ग ‘पारखमार्ग’ पर
चलने वाले कबीरपंथी थे। संस्कृत और अंग्रेज़ी दोनों से अनभिज्ञ होने के
कारण, हिन्दी भी बस पढ़ ही सकने के कारण, “पढ़े-लिखे” लोगों के मुहावरे में
नवलदास “अनपढ़” कहे जाएँगे। ठीक उसी तरह, जैसे उनके “ज्ञानीजी” को –
कबीर को- को “पढ़े-लिखे” लोग “अनपढ़” कहते आए हैं।
उन्होंने कबीर-बानी की जिस तरह व्याख्या की, उससे एकाएक लगा, “ अरे!
ये तो वैसी ही बातें कर रहे हैं, जैसी मुझे बचपन में सूझा करती थीं”।उन
दिनों, जब सहज-बोध तरह-तरह के शास्त्र-ज्ञान और विमर्शों से
आच्छादित नहीं हुआ था, मुझे लगता था : “ जो कुछ है, भीतर या बाहर, संसार भर
में, सब एक अखंड का ही पसारा है। इस अनादि-अनंत जगत के परे कौन परमात्मा
हो सकता है? कहाँ हो सकता है?”
वह कथा भी बरबस याद आ गयी: पंडित सर्वजीत काशी पधारे थे, कबीर को
शास्त्रार्थ में पछा़ड़ने का संकल्प लेकर। बैल पर लदी पुस्तकों के रूप में
अपना ज्ञान साथ लेकर। कबीर की पुत्री कमाली से ही पूछ बैठे रास्ता कबीर के
घर का। कमाली ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन चुटकी लेने से न चूकी -“ जन
कबीर का सिखरि घर, बाट सलैली गैल; पाव न टिकै पिपीलिका, लोगन लादै बैल”।
सलैली गैल- रपटीली राह- की याद ठीक ही दिलाई कमाली
ने। जहां चींटी तक के पांव टिकना मुश्किल हो, ऐसी राह पर अहंकार को बैल की
पीठ पर लाद कर जो चले, उस ज्ञानी के लिए, कबीर के ‘घर’— उनके भीतर-बाहर के
अनभय अनुभव—की राह रपटीली ही है। लेकिन जो इंसान ज्ञान का नाता अपने
आस-पास, भीतर-बाहर के साथ जोड़ सके, ‘जग बौराना’ की खबर लेने के साथ-साथ
ही, कुछ ‘आतमखबर’ भी रख सके,उसके लिए कबीर का तो क्या, कबीर के राम का घर
भी सहज प्राप्य हो जाता है-‘सहज सुभाय मिले रामराइ’।
भगत नवलदास बता रहे थे—मैं उनकी बानी को अपने शब्दों
में ढाल रहा था— सर्वव्यापी,अखंड चेतन का बोध मनुष्य मात्र का जन्मजात बोध
है। जीव ही चैतन्य है, और वही व्याप्त है सारे ब्रह्मांड में। इसे “जानने”
के लिए कहीं “बाहर” जाने की ज़रूरत नहीं। इस व्याप्ति को बखानने के लिए
ब्रह्म, ईश्वर, निर्गुण या राम जैसे नाम देने पड़ते हैं- यही नाम की महिमा
है।जीव चैतन्य की बेकली को कहने के प्रयत्न में ; जो कही नहीं जा
सकती, उस अकथ कहानी को कहने की जिद में ही वाणी की सार्थकता है। इस
सार्थकता का ही नाम कविता है।
ऐसा ही सहजात बोध है, मनुष्य-मात्र की समता का। जन्म
से न कोई ऊँचा होता है, न कोई नीचा। न्याय की कामना इस सहज समता-बोध की ही
परिणति है। केवल अपने या अपने जैसे लोगों के लिए ही नहीं, सबके लिए न्याय।
केवल अपने साथ न्याय की बात सोचना तो केवल अपने लिए विशेषाधिकार हथिया लेने
की वासना भर है। इस वासना से मुक्ति पाए बिना उस चैतन्य से रिश्ता कैसे
बनेगा जो ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है- जो कबीर को ‘जग-जीवन’ में यों
व्यापा प्रतीत होता है, ज्यों “पुहपन में बास”। चैतन्य की ब्रह्मांड
–व्याप्ति के बोध को ‘आध्यात्मिक’ और समता-बोध और न्याय-कामना को
‘सामाजिक’- सुभीते के लिए भले ही कह लें, किन्तु इनके बीच किसी मूलभूत
विरोध की कल्पना निराधार है।
समग्र अस्तित्व से जुड़ाव के अहसास को बनाए रखने को
जो व्याकुल है, उस जीव-चैतन्य की बेकली को ‘सबद’ देने के दुस्साहस में ही
कविता की महिमा है, और सबके लिए न्याय के संघर्ष में ही जीवन की सार्थकता।
तत्व की बात तो बस इतनी ही है, बाकी सब तो माया का पसारा है। इस तत्व को
जिसने समझा, उसने मर-मर कर जीने की-मरजीवा होने की- नियति का मानो स्वेच्छा
से वरण कर लिया।
नवलदास जी के साथ बतिया कर राहत महसूस की। अपनी तरह
सोचने वाला एक मनुष्य और मिला। पुरानी समस्या है, सोच-विचार का सार्थक
सहभागी खोज पाना। स्वयं कबीर की भी तो परेशानी यही थी—“ऐसा कोई न मिले
जासे कहूँ निसंक”।
लेकिन राहत के साथ ही महसूस हुई बेचैनी भी।
कबीर का विधिवत अध्ययन शुरु किए बीस बरस हो
चुके थे, जब नवलदास जी से मिला था। दस बरस और बीत चुके। बेचैनी बढ़ती ही
गयी है। सवाल कई हैं। नवलदास जैसों के देशज कबीर-विमर्श के साथ कबीर के
अध्येताओं ने कैसा रिश्ता बनाया है? कबीर के समय को किस तरह देखा है? उस
समय पर कबीर के प्रभाव को किस तरह समझा और समझाया है? कबीर के और हमारे समय
के बीच जो समय गुजर गया है, उसके प्रभावों और परिणतियों को कैसे बखाना है?
कबीर कहते हैं-‘कहे कबीर मैं पूरा पाया’।
क्या अर्थ है कबीर के पूरेपन का? उनकी ‘भावभगति’ का
सामाजिक अर्थ क्या है? उनकी सामाजिकता का आध्यात्मिक पहलू क्या है?
‘भीतर-बाहर सबद निरंतर’ की साधना करते हुए, जो पाया, उस की “अकथ कहानी” ही
तो कबीर ने अपनी बानी में कही है। क्या हम इस कहानी को सुनने की विनम्रता
नहीं जुटा सकते? कबीर की बानी को और उनके समय को अपने हिसाब से
तोड़ने-मरोड़ने की बजाय कबीर और उनके समय के पूरेपन तक पहुँचने का
साहस नहीं जुटा सकते? ऐसी विनम्रता और ऐसे साहस के सिवा,कबीर के
पूरेपन को समझने की प्रामाणिक विधि और क्या हो सकती है?
कबीर समाज पर टिप्पणी करने वाले कवि थे,जो रचनाकार
समाज के बारे में कुछ नहीं कहते, उनकी रचनाएं भी उनके समाज के बारे में कुछ
बताती हैं। क्या बताती है कबीर की कविता उनके समाज के बारे में? जिस समाज
से कबीर रूपक, उपमान और दृष्टांत ले रहे हैं, जिस समाज की वे आलोचना कर रहे
हैं, वह क्या वक्त की बर्फ में जमा हुआ सा समाज लगता है? जो समय कबीर की
बानी को उत्सुकता और सम्मान के साथ सुन रहा है उसे क्या ‘स्तब्ध मनोवृत्ति
का काल’ कहा जा सकता है?
जिस की अंत्येष्टि के लिए राजा और नवाब के बीच
तलवारें चलने की नौबत आ जाए, जिसके नाम पर पंथप्रवर्तन दामाखेड़ा में
संपन्न व्यापारी धर्मदास और काशी में विद्वान् ब्राह्मण सर्वजित (जो कबीर
के शिष्य होकर सुरतिगोपाल बन गए थे) कर रहे हों, जिसके पंथ के मठ
वाणिज्य-व्यापार के लिए विख्यात नगरों में स्थापित किए गए हों, जिसकी बानी
कई स्रोतों में संरक्षित हुई हो, जिसके पंथ का प्रभाव ओड़ीसा से लेकर
गुजरात और सिंध तक, जनसामान्य से लेकर राजसभाओं तक व्याप्त हो, उस
साधक की आवाज को क्या उसके समाज के हाशिए तक सीमित कहा जा सकता है?
कबीर की बानी और जीवन-कहानी के साथ विभिन्न
वक्ताओं-श्रोताओं ने जो नाते बनाए, उनका कबीर की कही ‘अकथ-कहानी
प्रेम की’ पर क्या असर पड़ा? कबीर की बानी का उनके ज़माने से लेकर आज तक,
कबीर के समाज पर क्या असर पड़ा? काशी के जुलाहे को विधवा ब्राह्मणी का
पुत्र कब और क्यों बनाया गया? कबीर के समकालीन और देशभाषा में पद रचने
वाले साधक-विचारक रामानंद को संस्कृत में भाष्य रचने वाले आचार्य रामानंद
में कब, किसके द्वारा, क्यों बदला गया? कब और क्यों रामानंद का समय कबीर से
पूरे सौ साल पीछे ले जाया गया? क्योंकर मुक्तिबोध को कबीर आधुनिक चित्त के
निकट लगते हैं? क्योंकर दिलीप चित्रे को तुकाराम मराठी के पहले आधुनिक कवि
लगते हैं?
कबीर को, और उनके समय को समझने के लिए, इन सवालों पर
तथ्यसम्मत और तर्कसंगत विचार करना जरूरी है। कबीर की ‘खोज’ या उन पर ‘शोध’
करने के पहले कबीर की लोक-स्मृति के साथ संवाद जरूरी है। कबीर के ही नहीं,
सभी समाजों के स्मृति-कोषों और औपनिवेशिक ज्ञानकांड द्वारा उनके उपयोग,
दुरुपयोग को समझना जरूरी है, ताकि हम इस ज्ञानकांड द्वारा इन समाजों में की
गयी “खोजों” की नवैयत समझ सकें।
2. स्मृति, खोज और देशभाषा
के स्रोतः किस्सा राजू गाइड का.
1828 ई0 में, ‘ए स्केच ऑफ रिलीजस सेक्ट्स ऑफ हिन्दूज’
के लेखक एच0एच0 विल्सन को लगा था कि कबीर किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम
नहीं, जेनेरिक संज्ञा, एक पदवी भर है। इस पदवी को धारण करने वाले न जाने
कितने लोगों ने ‘कबीर’ नाम से रचनाएँ की हैं। उत्तर भारत में एक खास
मिजाज की रचना को कबीर कृत बताया जा सकता है, और ये रचनाएँ इतनी संख्या में
तथा इतने विविध स्रोतों से मिलती हैं, कि हो न हो, कबीर अवश्य एक जेनेरिक
शब्द है, किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं। यह लिखने के बावजूद विल्सन ने
अपने पाठकों को कबीर के जीवन और बानियों से भी परिचित कराया और कबीर
पंथ से भी।
विल्सन की बात आधी सही है और आधी गलत। यह सही है कि
कबीर नाम से न जाने कितने लोगों ने रचना की है, लेकिन ‘कबीर’ सिर्फ
जेनेरिक शब्द, सिर्फ पदवी नहीं है। आधी सही-आधी गलत, विल्सन की यह बात,
पिछले दो सौ सालों में किए गए कबीर विषयक अध्ययनों की विडंबना जरूर
सामने ले आती है। इन दो सौ सालों में इतने सारे और इतने परस्पर विरोधी कबीर
हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं कि ऐतिहासिक कबीर तक पहुँचना नामुमकिन सा
लगने लगता है। व्याख्याओं की ऐसी विरोधी विविधता, तुलसीदास और दूसरे
सगुणमार्गी भक्तों के मामले में नज़र नहीं आती। तुलसीदास की कविता का
वैचारिक आशय और सामाजिक दिशा स्पष्ट है। यह स्पष्टता तुलसीदास के प्रगतिशील
प्रशंसकों को खासी उलझन में भी डालती रही है। दूसरी ओर, कबीर की संवेदना
में उत्तेजक बहुवचनात्मकता और उनके ज्ञानकोष में गहरी विविधता
है।
कबीर की कविता में प्रखर सामाजिकता और नितांत निजी
प्रेमानुभूति तेल और पानी की तरह नहीं, जल और बूँद की तरह दीख पड़ती हैं।
उनका ज्ञानकोष हिन्दू परंपरा और नाथपंथी साधना के साथ-साथ इस्लाम से
भी अच्छे खासे परिचय का प्रमाण देता है। थे वे जुलाहे परिवार के,
शिष्य-संवादी बने वैष्णव साधक रामानंद के। शाक्तों से कबीर की चिढ़ शाक्त
साधना से उनके गहरे परिचय का संकेत करती है। अनंतदास ‘कबीर-परिचई’
(1590 के आस-पास) में स्पष्ट कहते हैं कि कबीर शुरू में शाक्त रहे थे-‘बहुत
दिन साकत मैं गइया, अब हरि के गुन लै निरबहिया’।
‘जामें कुटुम समाए’ की प्रार्थना करने वाले गृहस्थ
कबीर की कविता में वैराग्य का स्वर भी कम प्रबल नहीं। ‘नारी पराई या आपनी’
के बारे में बेहद तीखी बातें करने वाले कबीर अपने राम के प्रति भक्ति और
प्रेम प्रकट करने के पलों में स्वयं नारी बन जाते हैं। उन्हें जितनी बेचैनी
‘बाहर’ को लेकर होती है, उतनी ही गहरी वेदना ‘भीतर’ को लेकर।
कबीर की काव्य-संवेदना रामभावना, कामभावना और
समाजभावना को एक साथ धारण करती है। इन तीनों के सर्जनात्मक सह-अस्तित्व को
पढ़े बिना, कबीर को पढ़ने के दावे व्यर्थ हैं।
जन्मजात सामाजिक पहचान के स्थान पर कबीर समान संवेदना
और मूल्य-बोध पर आधारित पहचान की खोज करते हैं, अपने लिए भी और अपने
श्रोताओं, संवादियों के लिए भी। इस ‘सामाजिक’ खोज में लगे होने के कारण
‘आध्यात्मिक’ खोज उन्हें बेमानी नहीं लगने लगती। उनके लिए ये खोजें
विरोधी नहीं, परस्पर निर्भर हैं। कबीर सामाजिक व्यवस्था, परंपरा और
मान्यताओं के रूपांतरण का प्रस्ताव करते हुए अपनी व्यक्ति सत्ता को
लगातार रेखांकित करते हैं- इसीलिए वे ‘आधुनिक मनुष्य को अपने चित्त के अधिक
निकट लगते हैं’।
‘निकट लगते हैं’, या वास्तविकता यह है कि “आधुनिकों”
को लगता है कि कबीर का “रणनैतिक उपयोग” आसानी से किया जा सकता है। कबीर को
निकट मानने वाले अधिकांश अध्येता अपने मनोवांछित उपकरण में उन्हें बदलने के
उत्साह में इस हद तक चले जाते हैं कि ऐतिहासिक कबीर की पहचान का सवाल ही
बेमानी हो जाता है।
लेकिन, आखिर कोई तो मनुष्य रहा होगा, जिसे पिछले दो
सौ सालों में किसी ने ईसाई मिशनरी के पूर्वपुरुष के रूप में देखा तो किसी
ने सूफी के रूप में। जिसे कोई हिन्दू धर्म की रक्षा का श्रेय देना चाहता
है, तो कोई जिसे हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए समर्पित मानता है। किसी के
अनुसार जिसने अपना निराला पंथ निकाला तो किसी के हिसाब से जो हिन्दू धर्म
और इस्लाम से सर्वथा स्वतंत्र नये धर्म का प्रतिपादन करना चाहता था। किसी
के अनुसार जो वैष्णव मत से थोड़ा प्रभावित लेकिन असल में लगभग नाथपंथी ही
था।
कबीर के ‘आधुनिक’ अध्ययनों का श्रीगणेश होने के बाद
से उन तक पहुँचने के जो रास्ते सुझाए गए हैं, उन पर चल कर आप उपरोक्त में
से किसी भी कबीर तक पहुँच सकते हैं। विल्सन के ‘जेनेरिक’ कबीर में रचनाओं
की बहुलता और रचना-रूपों की विविधता अवश्य थी, लेकिन वैचारिक और
संवेदनागत निरंतरता के साथ। व्याख्याकारों द्वारा प्रतिपादित कबीर छवियों
में विविधता से ज्यादा दिखता है- परस्पर विरोध। इन छवियों में से हर छवि
यदि सिर्फ एक ‘कंस्ट्रक्ट’ है, और सही ‘कंस्ट्रक्ट’ की पहचान सिर्फ ‘सही’
पॉलिटिक्स के आधार पर की जानी है तो फिर साफ-साफ कहिए कि कबीर असल में इस
धरती पर आए किसी हाड़-माँस के किसी इंसान का नाम नहीं, सिर्फ एक जेनेरिक
संज्ञा है। करना बस यही है कि इस संज्ञा में वह पॉलिटिक्स भर दें
जिसे आप सही मानते हों। कबीर की अपनी संवेदना तक पहुँचने में सर खपाने की
क्या जरूरत?
किसी भी कवि की विविध व्याख्याएं की जा सकती हैं।
विविधता विचारोत्तेजक होती है। लेकिन विविधता के नाम पर क्या तथ्यों की
पूर्ण उपेक्षा और व्याख्या के नाम पर मनमानेपन को जायज ठहराया जा सकता है?
‘सही’ पॉलिटिक्स में क्या इतनी भी दम नहीं होती कि कबीर को जबरन ‘ऑफिशियल
स्पोक्समैन’ बनाने की बजाय अपनी बात खुद कहे। ‘सही’ पॉलिटिक्स किसी समाज की
ऐतिहासिक स्मृति के साथ मनमानापन किए बिना काम क्यों नहीं चला सकती?
संतों-भक्तों की रुचि आत्मकथा लिखने में नहीं
‘आतमखबर’ जानने और जनवाने में थी। इसीलिए कबीर ही नहीं, इनमें से किसी के
बारे में भी शुद्ध अंतस्साक्ष्य के आधार पर ठेठ आधुनिक किस्म की
जीवनी-जिज्ञासा की तृप्ति तो असंभव है। लेकिन यह कतई नहीं कहा जा सकता कि
कबीर के समाज और समकालीनों ने उनका कोई नोटिस ही नहीं लिया और कबीर
की ‘खोज’ करने का काम “आधुनिकों” और उत्तर-आधुनिकों के ही भरोसे छोड़ कर चल
दिए।
कबीर का निधन देर से देर 1518 ईस्वी में माना जाता
है। पचास साल के भीतर-भीतर हरिराम व्यास ने उनके तथा उनके गुरु रामानंद के
गुण गाए। सौ साल के भीतर-भीतर अनंतदास ने कबीर की पूरी परिचई लिखी। परिचई
शब्द परिचय का आशय तो प्रकट करता ही है, साथ ही चमत्कार वर्णन का आशय भी इस
शब्द से व्यंजित होता है। कहावत है-‘देवी दिन काटे, पंडा परचा (चमत्कार का
प्रमाण) मांगे’। निधन के सौ बरस के भीतर ही कबीर की हैसियत चमत्कारी
शख्सियत की मान ली गयी थी। लेकिन “आधुनिकों” को कबीर असफल नजर आते हैं।
किसी को लगता है कि वे ‘मुसलमानों के बीच रह कर भगवान के दुष्टदलनकारी रूप
की बात करने का साहस न जुटा सके’, तो किसी को लगता है कि वे अलग धर्म की
स्थापना करना तो चाहते थे, कर नहीं पाए।
इन “आधुनिक” आकलनों के विपरीत भक्तमाल परंपरा का
सूत्रपात करने वाले नाभादास कबीर के गुण गाते हैं : ‘भक्तिविमुख धरम सु सब
अधरम करि गाये’। कबीर के कनिष्ठ समकालीन, गागरोन के राजा पीपा पहले ही कह
चुके थे-‘जो कलि नाम कबीर न होते तो लोक बेद और कलिजुग मिलि कर भगति रसातल
देते’। नाभादास के कुछ वर्ष बाद मुबाद शाह अपने ‘दबिस्ताँ-ए-मज़ाहिब’ में
‘वैष्णव वैरागी’ कबीर की ओड़ीसा तक व्याप्त लोक-मान्यता का संकेत करने के
साथ उनकी साधना के अनोखेपन का बखान भी कर रहे थे।
लेकिन कबीर के “आधुनिक” अध्ययन कबीर की ऐसी स्मृतियों
को कबीर की उस खोज के चश्मे से ही देखना पसंद करते हैं, जो यूरोपियनों ने
अपने हिसाब से की थी। खोज की ही जाती है विस्मृत या उपेक्षित की। सो, खोजना
यह चाहिए कि ये यूरोपियन कबीर की इतनी व्यापक लोक-स्मृति में से खोज क्या
रहे थे?
कबीर की व्यापक लोक-मान्यता के प्रत्यक्ष संपर्क में
पहले-पहल अंग्रेज़ अफसर और विद्वान नहीं बल्कि उत्तरी बिहार में आकर बसे
रोमन कैथॉलिक, इटालियन पादरी आए थे। उन्होंने कबीरपंथ का व्यापक प्रभाव
देखा। यह बात है, ईसा की अठारहवीं सदी की। यूरोप को कबीर के बारे में
पहले-पहल बताने का श्रेय मारको डेला टोंबा नामक पादरी को जाता है। कबीर के
व्यापक प्रभाव को तो यूरोपियन नकार ही नहीं सकते थे, इसलिए उनकी खोज चली
कबीर की “विस्मृत, उपेक्षित भूमिका” की ओर। “खोज” करके उन्होंने कबीर के
अपने समाज को को कभी बताया कि कबीर इस्लाम के प्रचारक थे, तो कभी बताया कि
ईसाई रहस्यवादियों सरीखे रहस्यवादी थे। देशी बौद्धिक ऐसी मान्यताओं से बहस
अवश्य कर रहे थे, लेकिन अधिकांश मामलों में औपनिवेशिक ज्ञानकांड की सीमाओं
के पार जाए बिना।
आधुनिक हिन्दी में कबीर पर, 1916 में पहली मुकम्मल
किताब लिखने वाले ‘हरिऔध’ वेस्टकॉट से बहस कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट पादरी
जी.एच. वेस्टकॉट ने अंग्रेजी में कबीर पर पहली मुकम्मल किताब, 1907 में
लिखी थी। पारंपरिक स्रोतों का उपयोग वेस्टकॉट ने भी किया था, हरिऔध
ने भी। लेकिन बहस के बिन्दु और उसकी सीमाएँ वही थीं जो वेस्टकॉट चाहते थे।
सफलता अकेले वेस्टकॉट की नहीं, औपनिवेशिक आधुनिकता की थी।
औपनिवेशिक आधुनिकता में रची-बसी ‘खोज-दृष्टि’ कबीर के
समाज की लोक-स्मृति को ही नहीं, स्वयं कबीर को भी ऐसी कृपादृष्टि से
देखती है जिसे कबीर अबोध बच्चे से नजर आते हैं, जो अपने घर का पता तक ठीक
से नहीं बता पाता। देखिए न, असल में तो वे थे— ईसाई मिशनरी के पूर्व-पुरुष,
शरा या बेशरा सूफी, महायानी बौद्ध, नाथपंथी या आजीवक, लेकिन समझते थे
खुद को नारदी भक्ति में मगन-‘ भगति नारदी मगन सरीरा-इहि विधि भव तरै
कबीरा’!
कबीर अकेले ही क्यों, ऐसे खोजियों के हिसाब से
तो सारा समाज ही एक तरफ ‘भोले-भाले’ अबोध लोगों और दूसरी तरफ सुबह से शाम
तक साजिश रचने वालों के बीच बंटा हुआ था। ‘भगति नारदी’ वाली पंक्ति तो ऐसे
साजिशी लोगों की ही करतूत ठहरी।
हालत यह है कि औपनिवेशिक आधुनिकता और उत्तर-आधुनिकता
की कृपा से कुछ लोगों की साजिशों और बाकी लोगों के बुद्धूपन को
भारतीय सांस्कृतिक अनुभव की ऐतिहासिक व्याख्या के बीज-शब्दों (की
कंसेप्ट्स) के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है।
कबीर को अंगुली पकड़ कर चलाने की बजाय, उनकी कविता
की अंगुली पकड़ कर चलें; विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और प्रमाणों के साथ
मनमानी करने की बजाय, उन्हें विवेक के साथ, समग्रता में पढ़ें, तभी हम कबीर
की संवेदना और उनके समय के बारे में प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच
सकेंगे। और बातों के अलावा यह भी जान सकेंगे कि कबीर कैसे ‘बहुत बरस
साकत मैं गइया’ से शुरु कर ‘भगति नारदी मगन सरीरा’ तक पहुंचे थे।
भारत ही नहीं, किसी भी समाज या परंपरा
के अनुभवों को साजिश और बुद्धूपन सरीखे ‘बीज-शब्दों’ (!) के जरिए नहीं
समझा जा सकता।
इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि संस्कृत और फारसी के समांतर देशभाषाओं
के बौद्धिक जगत में कबीर तथा अन्य लोगों पर विचार-विमर्श होता रहता था।
इस विचार-विमर्श की परंपरा औपनिवेशिक आधुनिकता के समांतर उन्नीसवीं सदी तक
जारी थी, अभी भी जारी है।
संस्कृत, फारसी के मुकाबले देशभाषा स्रोतों की
उपेक्षा औपनिवेशिक ज्ञानकांड में बद्धमूल थी और अभी भी है। इस बद्धमूल
संस्कार की मनोरंजक परिणतियां हम रामानंद-कबीर संबंध के प्रसंग में
देखेंगे। इसी संस्कार के कारण, उन्नीसवीं सदी के ‘पाखंडखंडिनी’ और
‘त्रिज्या’ के विवाद को, उन्हीं दिनों चल रही, कबीर की ‘खोज’ में, ध्यान
देने योग्य पाठ की हैसियत नसीब न हो सकी। बीजक की ‘पाखंडखंडिनी’ टीका
पारखमार्ग के प्रणेता पूरण साहब की ‘त्रिज्या’( 1837ई0) का खंडन करने के
लिए ही लिखी गयी है। ‘पाखंडखंडिनी’ के रचयिता विश्वनाथसिंह जू देव ने
चूँकि कुछ और काव्य-रचना भी की थी, सो शुक्लजी के ‘इतिहास’ में उनका उल्लेख
हुआ। उन्होंने कबीर को सगुण रामावतार का ही उपासक सिद्ध कर दिया था। यह चलन
बन गया कि कबीर के अध्येता ‘पाखंडखंडिनी’ पढ़ें न पढ़ें, उसका उल्लेख अवश्य
करें। ‘त्रिज्या’ के लेखक पूरण साहब भी खासे कल्पनाशील टीकाकार थे।
उन्होंने कबीर को जैनों जैसा ‘जीववादी’ सिद्ध कर दिया था। शायद इसीलिए वे
शुक्लजी को उल्लेखनीय न लगे हों। जो हो, ‘हरिऔध’ के बाद किसी “आधुनिक”
अध्येता ने ‘त्रिज्या’ को थोड़ी-बहुत चर्चा करने योग्य भी नहीं समझा।
हाँ, क्षितिमोहन सेन और केदारनाथ द्विवेदी जैसे कुछ विद्वानों ने
कबीर-पंथ के प्रसंग में ‘त्रिज्या’ का उल्लेख भर जरूर
किया।
‘खोज’ और ‘स्मृति’ के परस्पर संबंध का कबीर को समझने
पर क्या असर पड़ता है- यह आप इस पूरी पुस्तक में देखेंगे। आप यह भी देखेंगे
कि कबीर के अध्येताओं ने देशभाषा स्रोतों—रचनाओं या व्यक्तियों—की या तो
एकदम उपेक्षा की है, या फिर उनका उपयोग औपनिवेशिक ज्ञानकांड द्वारा “खोजी”
गयी किसी न किसी कबीर-छवि को “प्रामाणिक” सिद्ध करने भर के लिए, ‘नेटिव
इंफार्मेंट’ की तरह किया है। नेटिव इंफार्मेंट का मतलब हैः ऐसा व्यक्ति जो
अपने समाज के बारे में कुछ सूचनाएं अध्येता तक पहुंचाए। उससे यह उम्मीद
नहीं की जाती कि इन सूचनाओं का अर्थ समझे या उस पर
विचार-विमर्श कर सके। उसका काम सूचना देना भर है, विचार-विमर्श करने की
अक्ल उसमें कहां? सूचना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखने की सामर्थ्य उसमें
कहां?
देशभाषा स्रोतों को नेटिव इंर्फामेंट के रूप में
बरतने के पीछे इरादे अलग-अलग भी हो सकते हैं, लेकिन नतीजा एक ही है।
देशभाषा स्रोतों के साथ ऐसा बर्ताव करने के कारण ही ,उस ‘पिछड़े’ समय में
निर्गुण संतों का होना आश्चर्यजनक लगने लगता है। अपने समाज को दूर तक
प्रभावित करने वाले, दैनंदिन व्यवहारों में बदलाव ले आने में सफल होने वाले
साधक असफल सुधारक/ क्रांतिकारी लगने लगते हैं। सभी संगठित धर्मों की आलोचना
करके धर्मेतर अध्यात्म का प्रस्ताव करने वाले कबीर धर्मगुरु लगने लगते हैं।
यह बात समझ के बाहर हो जाती है कि कबीर हों या तुकाराम, अपने परिवेश की ही
उपज भी थे, और उसे रूपांतरित करने वाले ऐतिहासिक कर्त्ता( एजेंट) भी। ये
लोग ‘वक्त से पहले’ पैदा हो गए अनोखे प्राणी नहीं थे, अनोखापन उनके समय और
परिवेश में था, जिसने इन्हें इतने समर्थक और अनुयायी दिए।
देशभाषा स्रोतों को ‘भोले-भाले’, बल्कि अज्ञानी
‘नेटिव इंर्फामेंट’ की तरह बरतने के कारण, भारतीय चिन्तन परंपरा को संस्कृत
तक सीमित कर देने के कारण, चौदहवीं सदी से आरंभ हुए भक्ति-आंदोलन और
‘प्राचीन भागवत धर्म’ के अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह सवाल ही लोगों
के मन में नहीं उठता कि सोलहवीं सदी के अनंतदास आखिर क्यों और किस अर्थ मे
चौदहवीं सदी के नामदेव को ही कलियुग में भक्ति का प्रतिपादन करने का श्रेय
दे रहे थे—“ कलिजुगि प्रथमि नामदेव भइयो”।
अन्य वैष्णवों की तरह अनंतदास भी कलियुग का आरंभ
श्रीकृष्ण के गोलोकगमन के बाद से ही मानते रहे होंगे। ‘प्राचीन भागवत धर्म’
इस घटना के बाद ही आया था। लेकिन अनंतदास ‘प्राचीन भागवत धर्म’ को नहीं,
सैकड़ों साल बाद के, चौदहवीं सदी के नामदेव को कलियुग में भक्ति के
प्रतिपादन का श्रेय दे रहे हैं। विनांद कैल्वर्त्त जैसे लोग रामानंद को
कबीर का गुरु बताने के कारण अनंतदास के इतिहास-बोध पर तरस खाते हैं।
रामानंद, कबीर, पीपा और रैदास जैसों की भक्ति का आरंभ गुप्तकाल के
भागवत धर्म से नहीं, नामदेव की साधना से बताने वाले अनंतदास के भक्ति-बोध
पर ध्यान दें तो ऐसे लोगों के अपने बुद्धि-बोध का उद्धार होने की संभावना
बनती है।
अनंतदास बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं कि देशभाषाओं का
भक्ति-आंदोलन प्राचीन भागवत धर्म का पुनरोदय मात्र नहीं,उसकी परंपरा का
नवसंस्कार सूचित करता है। इस पर सिद्ध-नाथ प्रभाव अवश्य हैं, लेकिन इसकी
अपनी विशिष्ट पहचान तो नामदेव से ही आरंभ होती है।
देशभाषा स्रोतों पर ध्यान देने से पता चलता है कि
जुलाहे कबीर, कुनबी तुकाराम, दर्जी नामदेव, सुनार अखा और चर्मकार रविदास
की उपेक्षा अंग्रेजी से वंचित समाज ने नहीं, बल्कि अंग्रेजी ढंग पर खडे़
किए गए विश्वविद्यालयों ने की। जहां तक समाज का सवाल है, कबीर पर ब्रिटिश
प्रशासकों और विद्वानों का ध्यान गया ही इसलिए कि उन लोगों ने सारे उत्तर
और मध्य भारत में कबीर को पुजते पाया। इन में विल्सन जैसे धार्मिक
संप्रदायों का इतिहास और ग्रियर्सन सरीखे ‘देशी’ साहित्य (वर्नाक्युलर
लिट्रेचर) का इतिहास लिखने वाले ही नहीं, विलियम क्रुक जैसे समकालीन
जाति-व्यवस्था का विवरण लिखने वाले भी शामिल हैं। क्रुक का विवरण पहले ‘दि
ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ-वेस्टर्न प्राविन्स ऐंड अवध’ शीर्षक से
प्रकाशित हुआ था। बाद में इसी के विस्तृत रूप का प्रकाशन 1896 में ‘ दि
ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया’ नाम से हुआ। कबीरपंथियों
के बारे में लिखते हुए क्रुक लिखते हैं, “तुलसीदास की रामायण को छोड़ कर
शायद किसी भी अन्य रचना को उत्तर भारत के हिन्दुओं के बीच वैसी लोकप्रियता
हासिल नहीं है, जैसी कबीर के बीजक को। उनकी बानियाँ तो हिन्दू या मुसलमान
सभी के मुँह से कभी भी सुनी जा सकती हैं”।[i]
क्रुक के कोई आधी सदी बाद, और अब से कोई आधी सदी
पहले, ‘उत्तराखंड में संतमत और संतसाहित्य’ के बारे में लिखते हुए, डॉ0
पीतांबरदत्त बड़थ्वाल कबीर-महिमा के बारे में बता रहे थे कि उत्तराखंड में
कहीं-कहीं कबीर को नाथ ही माना जाता है, और “नरंकार की पूजा में कबीर
की जागर लगती है”।[ii]
‘जागर’ कहते हैं, किसी व्यक्ति में किसी देवता का
आवेश आमंत्रित करने को।
कबीर समाज में पुजते हैं और पुजते थे। सवाल यह है:
वो कौन सी सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाएँ थीं जिन्होंने परजीवी ब्राह्मणों और
मुल्लाओं की लाख चिल्ल-पों के बावज़ूद कबीर और दूसरे संतों को पूज्य बनाया?
यह भी जग-जाहिर है कि निर्गुण-पंथी संतों में से अधिकांश दस्तकार थे। सवाल
यह है: इन लोगों को प्राप्त लोक-मान्यता में व्यापार की, व्यापार से जुड़े
लोगों की क्या भूमिका थी? दस्तकारों की तादाद में बढ़ोत्तरी क्या व्यापार
के विस्तार के बिना संभव है? सामंती मनमानी के विरुद्ध फेयर-प्ले --
न्यायसंगत व्यवहार—की माँग दुनिया भर के इतिहास में व्यापार के विकास और
व्यापारियों के सामाजिक प्रभाव के विस्तार से जुड़ी हुई रही है। भारत क्या
इस विश्व-व्यापी वास्तविकता का अपवाद था? सचाई तो यह है कि निर्गुण
संवेदना की केन्द्रीय विशेषता (आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में
फेयर-प्ले की माँग) का सीधा संबंध व्यापारियों के सामाजिक अनुभवों और
आकांक्षाओं से जुड़ता था। इसी जुड़ाव के कारण परजीवियों द्वारा उत्पीड़ित
ये संत व्यापारियों और दस्तकारों के बीच पुजने की हद तक लोकप्रिय हुए।
कबीर और उनके समय को समझने के पहले,औपनिवेशिक
आधुनिकता द्वारा उनकी ‘खोज’ के निहितार्थों को समझना जरूरी है। “आधुनिक”
ज्ञानकांड उपनिवेशीकृत समाज के अपने स्मृति-कोष और स्मरण-विधियों से संवाद
करके इतिहास नहीं लिखता था। उसे जो चाहिए था, वह उपनिवेशीकृत समाज के अतीत
और वर्तमान में ‘खोज’ लेता था और सामाजिक स्मृतियों का उपयोग बस अपनी
‘खोज’ को जायज ठहराने के लिए करता था—अभी भी करता है। संस्कृत
साहित्य और भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येता शैल्डॉन पोलक ने यूरोपीय
अध्येताओं की पद्धतियों में अब तक प्रकट-अप्रकट जड़ें जमाए बैठे
‘ओरियंटलिज्म’ की चर्चा करते हुए याद दिलाया हैः “ इतिहास में ज्ञानकांड का
यह विरोध (‘पैराडॉक्स’) अनेक बार प्रकट हुआ है कि औपनिवेशिक थ्योरी
ने पूर्व— ओरियंट— के प्राचीन इतिहास में वे ही चीज़ें ‘खोज’ निकालीं,
जिनकी रचना असल में औपनिवेशिक सत्ता ने खुद ही की थी”।[iii]
ऐसी ‘खोजों’ के प्रभावों से मुक्त होकर सही सवालों
तक पहुँचने के लिए भारतीय इतिहास के बारे में रचे गए औपनिवेशिक
अंधविश्वासों से मुक्ति आवश्यक है। इन अंधविश्वासों की रचना के अपने
ऐतिहासिक संदर्भ और इन की परिणतियों का बोध आवश्यक है। इस दिशा में
कुछ प्रयत्न आप अगले अध्याय—‘संतो, जागत नींद न कीजै’—में पाएंगे। देशभाषा
स्रोतों से संवाद करने की परिणतियां तो आप इस पुस्तक में पन्ने-पन्ने पर
देखेंगे ही।
कबीर ही नहीं, भारतीय इतिहास लेखन मात्र के प्रसंग
में, परिचई के लेखक अनंतदास से लेकर त्रिज्या-टीका रचने वाले पूरन साहब तक
सरीखे देशभाषा के बौद्धिकों के साथ जो संबंध “आधुनिक” अध्येताओं ने
बनाया है, वह याद दिलाता है, फिल्म ‘गाइड’ के एक दृश्य की। राजू गाइड को
गांव वाले साधु-महात्मा समझने लगे हैं। गांव के पुरोहितों को राजू का
सम्मान नागवार गुजरता है। वे संस्कृत बोलने की चुनौती देकर राजू को साधु
नहीं, अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं—“ बोलेंगे क्या, संस्कृत आती
हो तब ना!” राजू गाइड की नाक का सवाल है। वह अंग्रेजी बोलने लगता है, और
पुरोहितों को अज्ञानी सिद्ध कर देता है—“बोलेंगे क्या, अंग्रेजी आती हो तब
ना!”
जो न संस्कृत या फारसी बोलते हैं, न अंग्रेजी, वे
“बोलेंगे क्या?” –इस मानसिकता से मुक्त होकर सुनें तो हम सुन सकते हैं कि
कबीर को उनके समाज और परंपरा ने न असफल स्वर माना न हाशिए की आवाज। हम यह
भी देख सकते हैं कि कबीर के समय का भारत उद्धार के लिए यूरोपीय आधुनिकता के
अवतार की प्रतीक्षा करता भारत नहीं, स्वयं अपनी परंपरा से पनप रही आधुनिकता
की ओर बढ़ता भारत था। कबीर और तुकाराम आधुनिक इसलिए नहीं लगते कि वे अपने
समय से आगे निकल कर आधुनिक हो गए हैं, बल्कि इसलिए लगते हैं क्योंकि जिस
समय में ये कवि रचना कर रहे हैं, वह समय भारतीय इतिहास में आधुनिकता के उदय
का समय है।
आप इस किताब में देखेंगे कि कबीर के समय और भारतीय
सांस्कृतिक अनुभव के बारे में मेरी धारणाएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं; कारण
यही है कि पिछले कई सालों से मैंने संस्कृत और अंग्रेजी के साथ उन ऐतिहासिक
और समकालिक स्रोतों को भी पढ़ने, सुनने और गुनने की कोशिश की है, जो न
संस्कृत, फारसी बोलते हैं, न अंग्रेजी।
3. आधुनिकताः देशज बनाम
औपनिवेशिक
कबीर और रामानंद ईसा की पंद्रहवीं-सोलहवीं सदी में
सक्रिय थे। ‘रामचरितमानस’ की रचना 1574ई0 में हुई, 1582 में ‘पद सूरदासजी
का’ नामक संकलन तैयार किया गया। नाभादास ने ‘भक्तमाल’ 1585 से 1620 के बीच
रची। अनंतदास ने अपनी परचइयां 1588 से 1600 के बीच रचीं। 1604 में
‘आदिग्रंथ’ को अंतिम रूप दिया गया। धर्मदास ने कबीरपंथ की स्थापना सत्रहवीं
सदी के आरंभ में की। इसके पहले वल्लभाचार्य, दादू और चैतन्य के संप्रदाय
स्थापित हो चुके थे। विभिन्न संप्रदायों में निर्गुण-सगुण की आत्मचेतना
सत्रहवीं सदी के मध्य से साफ दिखने लगती है—लेकिन उतने कठोर और परस्पर
अपवर्जी रूप में नहीं, जितनी आ0 शुक्ल के काल और प्रवृत्ति-विभाजन से
प्रतीत होती है। ‘पद सूरदासजी का’ में सूरदास के ही नहीं, नामदेव और कबीर
के पद भी हैं।
पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में घट रही
उपरोक्त सांस्कृतिक घटनाओं का सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक परिवेश से कोई
संबंध था या नहीं? उस परिवेश के स्वरूप को समझे बिना क्या इन घटनाओं का
सामाजिक अर्थ और ऐतिहासिक महत्व समझा जा सकता है? इन घटनाओं की तर्कसंगत
व्याख्या किए बिना क्या उस ऐतिहासिक परिवेश को तर्कसंगत ढंग से ‘पढ़ा’ जा
सकता है?
सवाल इतिहास से भी जुड़े हैं, वर्तमान और भविष्य से
भी।
इमेनुएल वार्लस्टाइन ने ‘इक्कीसवीं सदी के लिए
समाज-विज्ञान का एजेंडा’ बनाने की कोशिश में किताब लिखी हैः ‘दि एंड ऑफ दि
वर्ल्ड ऐज वी नो इट’। चुनौती को बिल्कुल ठीक समझा है वार्लस्टाइन ने। कहते
हैं: बतौर ऐतिहासिक व्यवस्था के, आधुनिक
विश्व-व्यवस्था का अंत निकट है। यह पचास साल से अधिक नहीं चलने वाली। लेकिन
पता नहीं कि जो व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था की जगह लेगी, वह इससे बेहतर होगी
या बदतर। इतना तय है कि संक्रमण-काल बेइंतिहा तकलीफों से भरा होगा, क्योंकि
इतना कुछ दांव पर है। नतीजे बिल्कुल अनिश्चित हैं और छोटी-छोटी चीजें भी उन
नतीजों पर गहरा, दूरगामी असर डाल सकती हैं।[iv]
इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि विधाता ने इतिहास को किसी पूर्व-निर्धारित
मार्ग पर चला कर उस मार्ग का नक्शा कुछ चुनिंदा लोगों के कान में नहीं
फूँक दिया है। बेहतर भविष्य बंद गली का आखिरी मकान नहीं है कि ‘राह
पकड़ कर एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला’! आने वाली व्यवस्था बेहतर हो, इसके
लिए सोचना जरूरी है कि बीते वक्त को समझने में क्या कमियां रह गयीं। अतीत
का बेहतर बोध बेहतर भविष्य की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी ओर बढ़ने
में मदद जरूर कर सकता है। अपने देश में जो लोग बेहतर भविष्य चाहते हैं, वे
अभी कुछ बरस पहले तक जाति का गंभीर विमर्श तक नहीं करते थे, और इन दिनों
सिर्फ जाति का ही विमर्श करते हैं। पहले मानते थे कि जाति जैसे है ही नहीं,
अब मानने लगे हैं कि बस जाति ही जाति है, बाकी कुछ भी नहीं है।
पेंडुलम-धर्म का निर्वाह इतनी निष्ठा से किया जा रहा है कि देख कर मजा आ
जाता है।
कबीर को ही नहीं, समूचे भारतीय अनुभव को समझने और
उससे सीखने के लिए ‘पेंडुलम-धर्म’ से मुक्ति आवश्यक है। कबीर के
ऐतिहासिक परिवेश के बारे “सहज” सत्य मान लिए गए कुछ असत्यों से
मुक्ति आवश्यक है। यह किताब ऐसे कुछ असत्य और उनकी समीक्षा आपके सामने
रखेगी।
आवश्यक है कि कविता को बतौर कविता के, संवेदनशीलता और
सम्मान के साथ पढ़ा जाए। सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानने-समझने के लिए
भी कविता को पढ़ना चाहिए। पहले से तय कर लिए निष्कर्षों को सिद्ध करने भर
के लिए कविता को पढ़ना व्यर्थ है। कबीर हों या कोई और कवि—उन्हें ‘इतिहास
की अदालत’ में अपने मुकदमे के गवाह के तौर पर बरतने भर से कविता के प्रति
संवेदनहीनता तो प्रकट होती ही है, इतिहास-लेखन की अपनी भी हानि होती है।
सामाजिक सत्तातंत्र और समाज की गतिशीलता के दैनंदिन जीवन-व्यवहार के उन
संकेतों को ‘पढ़ना’ चाहिए जो कबीर, तुलसी और मीरा जैसे रचनाकार अपनी
रचना में छोड़ गए हैं। इतिहास-लेखन के अन्य स्रोतों से इनकी तुलना
करके हम इन कवियों के बारे में ही नहीं, उनके देश-काल के बारे में भी कहीं
ज्यादा प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं।
इन दिनों इतिहासकार और समाजशास्त्री किसी भी समाज का
अध्ययन और मूल्यांकन दैनंदिन जीवन-व्यवहार -‘एवरीडे प्रैक्टिसेज़’-
के साक्ष्यों के आधार पर करने की बात करते हैं। मतलब यह कि ‘ऐसा होना
चाहिए’ कहने वाले शास्त्रों की तुलना ‘ऐसा होता है’ की सूचना देने वाले
स्रोतों के साथ करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाए। बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन, भारतीय समाज के अध्ययन के प्रसंग में इस पर अमल कितना होता है?
दैनंदिन व्यवहार के साक्ष्य देने वाले देशभाषा
स्रोतों की बात सुनें-समझें तो मालूम पड़ता है कि भारतीय समाज पर
ब्राह्मणों के निरंतर वर्चस्व की तस्वीर वास्तविक जीवन के अध्ययन पर नहीं,
निराधार फार्मूलों पर आधारित है। हिन्दी-क्षेत्र के बारे में तो निश्चित
रूप से कहा जा सकता है : शाश्वत ब्राह्मण-वर्चस्व की तस्वीर औपनिवेशक सत्ता
के साथ ब्राह्मणों के ‘कोलैबोरेशन’ के फलस्वरूप अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में
गढ़ कर कबीर के समय पर चिपका दी गयी है। इसीलिए, जिन्हें निकोलस डर्क्स
“ऑफिशियल ब्राह्मण”[v]
कहते हैं, उपनिवेशवाद के साथ उनकी जुगलबंदी के नतीजों को समझे बिना
ब्राह्मणवाद को न तो समझा जा सकता है, न उसका उचित उपचार किया जा सकता है।
तुलसीदास का कलिकाल वर्णन बताता है कि उनके
समय में व्यापार के कारण नयी जातियां बन रही हैं, वर्ण-व्यवस्था को
चुनौती मिल रही है। नवोदित जातियों को उनकी आर्थिक ताकत के आधार पर “उच्च”
मानने के लिए वर्ण-व्यवस्था के समर्थक विवश हैं। विवश वे तलवार की ताकत
वालों को ‘क्षत्रिय’ मानने के लिए भी हैं- भले ही कल तक उन्हें ‘निम्न
कुलोत्पन्न’ मानते रहे हों। विवश वे ‘वर्णाश्रम-बाह्य’ गोंडों को सफल राजा
बनते देखने के लिए भी हैं। विवश वे शूद्रों को गुरु के रूप में समादृत
देखने के लिए भी हैं। और ऐसी बहु-आयामी विवशता को ही वे “कलियुग” नाम दे
रहे हैं- व्यापार के विकास का वह समय उन्हें “धरम की हानि” का समय दिख रहा
है, जिसमें शूद्र ब्राह्मणों को डाँट रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों से जिरह
करने की हिम्मत कर रही हैं, और आदिवासी गोंड छत्रधारी राजा बन रहे हैं।
दैनंदिन व्यवहार की वास्तविकता तो “मध्यकालीन”
तुलसीदास के कलिकाल-वर्णन से झलकती है, लेकिन “आधुनिक”
सिद्धांत और ‘इतिहास लेखन’ ऐसे समकालीन स्रोतों की परवाह किए बिना ‘बताता’
है कि उस समय के समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता कर्मकांड तक सीमित न
होकर समाज के हर क्रिया-कलाप में अबाध रूप से स्थापित थी।
तुलसीदास का कलियुग संबंधी विलाप अभूतपूर्व नहीं है।
भारतीय इतिहास में जब-जब सामाजिक गतिशीलता दिखती है, तब-तब कलियुग- विलाप
भी दिखता है- ‘विष्णुपुराण’ से लेकर ‘रामचरितमानस’ तक। यह विलाप दैनंदिन
जीवन की परिवर्तनशालता को बताने वाला और ब्राह्मणों के अबाध, निरंतर
वर्चस्व के मिथकों को तोड़ने वाला साक्ष्य है।
कलियुग पर कोप करते तुलसीदास समाज की गतिशीलता को ही
रेखांकित कर रहे हैं। यही रेखांकन इस तथ्य में भी है कि
ब्राह्मण-वर्चस्व और संस्कृतकेन्द्रिकता को चुनौती देते रामानंद
‘जात-पांत पूछे नहीं कोई’ की घोषणा देशभाषा में कर रहे हैं। यह घोषणा
हिन्दू परंपरा में, वर्ण-व्यवस्थापरक के स्थान पर वर्ण-व्यवस्था विरोधी
सामाजिकता और धार्मिकता के प्रस्ताव की घोषणा है। आत्मालोचन और रूपांतरण का
न्यौता है— देशभाषा में किया जा रहा यह प्रस्ताव, और दैनंदिन व्यवहार में
रूपांतरण हो भी रहा है।
देशभाषाओं की प्रतिष्ठा ईसा की ग्यारहवीं सदी के बाद
से सारे भारत में ही नहीं, सारे यूरोप और एशिया में लक्ष्य की गयी है। इस
दौर में, यूरोपीय और गैर-यूरोपीय समाज अपने-अपने ढंग से आधुनिकता की ओर बढ़
रहे थे। भारतीय समाज कोई इतिहास-विहीन समाज नहीं था, जैसा हीगेल को लगा था।
वह भी तत्कालीन यूरोप की तरह इतिहास के रास्ते पर ही चलता हुआ समाज था।
यूरोप और भारत में यह समानता थी। फर्क यह था कि यूरोपीय साम्राज्यवाद के
कारण भारत और अन्य गैर-यूरोपीय समाजों में देशज आधुनिकता के सहज, आंगिक
विकास में बाधा पड़ी। भारत जैसे उपनिवेशीकृत समाजों में देशज आधुनिकता
अवरुद्ध हो गयी। औपनिवेशिक स्थिति के फलस्वरूप आई आधुनिकता ने परंपरा के
प्रवाह में आने वाले आवेग के स्थान पर परंपरा से तीक्ष्ण टूटन का रूप ले
लिया। परंपरा और आधुनिकता के बीच संवेदना-विच्छेद उत्पन्न हो गया। इन
समाजों की अनेक समस्याओं के मूल में यह संवेदना-विच्छेद ही है। कबीर के
प्रसंग में इसी संवेदना-विच्छेद के कारण निराधार बातों को ‘ऐतिहासिक
सचाइयों’ का दर्जा दे दिया गया है। कबीर को हाशिए की आवाज मानना ऐसी ही
निराधार बात है।
हाशिए पर ही रहे होते तो गागरोन के राजा पीपा यह न
कहते कि लोक, वेद और कलियुग से भक्ति को कौन बचाता, ‘जो कलि
नाम कबीर न होते’। उनके “कुप्रभाव” का निवारण करने के लिए वैसे आक्रमण करने
की जरूरत भी नहीं पड़ती,जैसे तुलसीदास ने किए हैं। संस्कृत स्रोतों को भी
ध्यान से देखने पर, यह काल ‘स्तब्ध मनोवृत्ति’ का काल नहीं लगता। व्यापक
सामाजिक गतिशीलता के प्रमाण आरंभिक औपनिवेशिक दौर के स्रोतों में भी मिलते
हैं। पता लगता है कि वाणिज्य के विस्तार के कारण, नित नयी जातियां बन रहीं
थीं। सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर-नीचे हो रहीं थीं। ये जातियां पेशों पर
आधारित थीं, ‘रक्त-शुद्धि’ पर नहीं। जातियों को रक्त-शुद्धि के नस्लवादी
सिद्धांत से जोड़ा—औपनिवेशिक आधुनिकता और उसके ज्ञानकांड ने।
वर्णाश्रम का सैद्धांतिक ढांचा सरल, बुनियादी
श्रम-विभाजन के दौर में विकसित हुआ था, फिर उसे एक ‘मॉडल’ या ‘नॉर्म’ बना
दिया गया। व्यापार के फलस्वरूप पनप रही नयी नयी जातियों को वर्णाश्रम
के मॉडल में फिट करना वर्णाश्रमपरक चिंतन की मुख्य समस्या बन गयी। यह बात
आठवीं सदी से ही देखी जा सकती है। इसी वक्त से शास्त्रीय
‘आर्षवाक्यों’ पर ‘लौकिक’ व्यवहारों को वरीयता देने की प्रवृत्ति भी दिखने
लगती है। मध्यकालीन निबंधग्रंथो के लेखकों की सोच स्थानीय लोक-व्यवहार को
शास्त्रानुरूप सिद्ध करने की थी—इस बात की ओर आ0हजारीप्रसाद द्विवेदी ने
बहुत पहले ध्यान खींचा था। युवा संस्कृतज्ञ आशुतोषदयाल माथुर ने पिछले
दिनों सप्रमाण दिखाया है कि आठवीं से चौदहवीं सदी तक के निबंध-ग्रंथों के
लेखक और पारंपरिक ग्रंथों के टीकाकार राजसत्ता को फालतू की वस्तु नहीं
मानते थे। वे तो, राजसत्ता को सामाजिक सत्ता के अन्य सभी रूपाकारों की
वैधता का आदिस्रोत सिद्ध करने में लगे थे। सामाजिक व्यवहार के नियमों
का प्रदाता भी वे राजा को ही निरूपित करते हैं, और दंड-विधान के जरिए
नियम-पालन कराने का एकाधिकार भी राजा का ही बताते हैं।[vi]
अंग्रेजी राज के पहले के भारत के संदर्भ में
‘पॉलिटिकल इकॉनॉमी’ की बात करने तक को कुछ लोग व्यर्थ मानते हैं। उनके
अनुसार उस समय के भारत का सामाजिक संगठन तो जजमानी पर ही आधारित था। और ऐसा
आठवी सदी ईसापूर्व से चला आ रहा था, उन्नीसवीं सदी ईस्वी तक चलता रहा। यह
शुद्ध अंधविश्वास है। किसी भी समाज की तरह भारत में भी, व्यापार भी था, और
‘पॉलिटिकल इकॉनॉमी’ भी। ईसा की आठवीं सदी के बाद से तो धर्मशास्त्रीय चिंतन
की मुख्य चिंता ही राजसत्ता की व्यावहारिक महत्ता को सैद्धांतिक रूप से
“शास्त्रसम्मत” भी सिद्ध करने की हो जाती है। लौकिक की वरीयता को,
धर्मशास्त्र को दैनंदिन व्यवहार के अनुरूप ढालने की प्रवृत्ति को,
समाज में राजसत्ता की व्यावहारिक शक्ति को “शास्त्रसम्मत” सिद्ध करने
के इस प्रयत्न को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र याद करते हुए, आशुतोषदयाल माथुर
सही नाम देते हैं: “धर्मशास्त्र का अर्थशास्त्रीकरण”।
‘धर्मशास्त्र के अर्थशास्त्रीकरण’ के इस काल में
वैष्णव प्रभाव बढ़ रहा था। स्मार्त्त और वैष्णव चिन्तन में
महत्वपूर्ण अंतर था। स्मार्त्त चिन्तन का बल ‘सार्वत्रिकता’ पर था। वह
क्षेत्रीय निबंध-ग्रंथों को महत्व देते हुए भी, “प्रमाण” अखिल-भारतीय,
सार्वत्रिक स्मृतियों को ही मानता है। दूसरी और वैष्णव सोच वैष्णव
पुराणों और संहिताओं को भी स्मृतियों के बराबर ही “प्रमाण” मानती है।
‘सार्वत्रिकता’ से अधिक वैष्णव चिन्तन स्थानीयता का सम्मान करता है। वैष्णव
पुराणों और संहिताओं पर गहरे क्षेत्रीय प्रभाव हैं। स्मृति और वैष्णव
संहिता या आचार्य के कथन में विरोध होने पर वैष्णव लोग वैष्णव स्रोतों को
ही प्रमाण मानते हैं। ये स्रोत स्थानीय व्यवहारों, परंपराओं को
शास्त्रसम्मत सिद्ध करते हैं; शास्त्र में व्यक्त होने वाली सार्वत्रिकता
के साथ किसी क्षेत्र या समुदाय के अपने स्वत्व का संतुलन बैठाने की उनका
यही तरीका है। रामानंद द्वारा रचित माना जाने वाला ‘वैष्णव मताब्ज भास्कर’
स्पष्ट निर्देश देता है कि मुक्ति के इच्छुक द्विजों को अद्विज वैष्णवों की
भी चरण-वंदना करनी ही चाहिए। यह रामानंदी संप्रदाय के स्वत्व का, उसके
वैशिष्ट्य का रेखांकन था। इसके विपरीत स्मार्त्त सोच का तरीका ऐसे
स्वत्व की उपेक्षा कर, सभी लोक-व्यवहारों को सार्वत्रिक शास्त्रीयता के
अनुकूल बनाने का है।
स्थानीय रंगत और लोक-जीवन में रचे-बसे वैष्णवों के
सामाजिक व्यवहार को ‘श्रुति-स्मृति’ सम्मत, ‘सार्वत्रिक’ वर्ण-व्यवस्था के
अनुकूल बनाने के लिए स्मार्त्त ब्राह्मण अनवरत प्रयत्न करते रहे। स्मार्त्त
प्रभाव में आकर दक्षिण में विजयनगर और उत्तर में जयपुर के राजाओं ने वैष्णव
संप्रदायों के सत्ता-तंत्र से शूद्रों को बाहर करने के लिए काफी कोशिशें
कीं। विजयनगर की कोशिशें सफल भी हुईं, लेकिन जयपुर की कोशिशें रामानंदीय और
कुछ अन्य वैष्णव संप्रदायों के संदर्भ में, कुल मिला कर असफल ही रहीं। इनके
विपरीत रामानुजी वैष्णव वस्तुतः ‘स्मार्त्त वैष्णव’ ही बन गए। वर्णाश्रमवाद
की विचारधारा उन्होंने पूरी तरह अपना ली। तुलसीदास ऐसे ही ‘स्मार्त्त
वैष्णव’ थे। बीसवीं सदी के रामानंदी वैष्णवों में भगवदाचार्य ने और
साहित्यकारों में से आ0रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की यह विशेषता बिल्कुल
ठीक लक्ष्य की थी। शुक्लजी का ध्यान ‘एक बात की ओर’ गया थाः
तुलसीदास जी रामानंदी संप्रदाय की वैरागी परंपरा में
नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्यपरंपराएँ मानी जाती
हैं उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में संमिलित
करने के लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह
कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त्त वैष्णव
थे।[vii]
हिन्दी क्षेत्र में प्रभावी रामानंदीय
वैष्णवता रामानुजीय, स्मार्त्त वैष्णवता से अलग हुई ही थी, “जात-पांत पूछे
नहीं कोई” की घोषणा के कारण। रामानंदीय वैष्णवता कबीर के समय से ही तथाकथित
“निम्न जातियों” के आत्मरेखांकन का माध्यम बन गयी थी।
उन्नीसवीं सदी में विलियम क्रुक ने देखा कि “ नित नयी
बनती रहने वाली पेशेवर जातियों में से लगभग सभी वैष्णव परंपरा के
किसी न किसी रूप से जुड़ी हुईं हैं”।[viii]
क्रुक का आशय रामानंदी वैष्णवता से ही था। (स्मार्त्त) वैष्णवता बनाम
(रामानंदी) वैष्णवता की चर्चा का अवसर हम रामानंद-कबीर संबंध के
प्रसंग में, और अन्यत्र भी पाएंगे।
अन्य समाजों की तरह, भारत में भी, औपनिवेशिक आधुनिकता
के आने के पहले के आरंभिक आधुनिक काल के सामने चुनौती पारंपरिक चिंतन और
सामाजिक स्मृति की निरंतरता बनाए रखने की भी थी। व्यापार के विस्तार के
कारण नित नई पैदा हो रही जातियों के प्रसंग में पद्धति यह बनी कि किसी जाति
को पेशे के आधार पर चार में से एक वर्ण के अंतर्गत रख दिया जाए, और इस रखाव
की व्याख्या किसी पौराणिक संदर्भ के आधार पर कर दी जाए। इस व्यावहारिक सोच
में कर्मकांड और पौरोहित्य (रिचुअल) भी ज़रूरी फंक्शन था, जो कि ब्राह्मण
जाति का काम था। ब्राह्मण की ‘पूज्यता’ और सर्वोच्चता दैनंदिन जीवन की
निरंतर सचाई कम, कर्मकांड के क्षण-विशेष की सचाई अधिक थी।
व्यावहारिक सचाई तो यह आज के जनजीवन की भी है,बशर्ते
हम औपनिवेशिक ज्ञानकांड द्बारा ब्राह्मणों के सहयोग से रचित ‘थ्योरी’
के मोह से मुक्त हो सकें। श्राद्धपक्ष में अपने ब्राह्मण मुनीम के पुत्र के
पांव छू लेने वाले सेठजी रोजमर्रा के जीवन में मुनीम का आज्ञापालन
नहीं करने लगते। ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि किसी राजा या सामंत को कर्मकांड
के लिए ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ी, पर्याप्त संख्या में मिले नहीं, तो राजा
साहब ने किसी पूरी की पूरी जाति को जनेऊ पहना कर रातोंरात ज़रूरत भर
ब्राह्मण पैदा कर लिए। कुछ समय तक अन्य ब्राह्मण ऐसे गढे़ गए ब्राह्मणों को
मान्यता देने में सकुचाते रहे, लेकिन दो-चार पीढ़ी बाद सब ठीक हो गया।
भारतीय समाज सामाजिक वरीयता का निर्धारण वास्तविक,
व्यावहारिक ताकत के आधार पर करता था,कोरी कर्मकांडपरक(रिचुअलिस्टिक) उच्चता
के आधार पर नहीं। कर्मकांडपरक वरीयता के कारण ब्राह्मण हर हाल में,
सर्वोच्च माने जाते थे; भारतीय समाज में सामाजिक शक्ति तलवार या पैसे से
नहीं, रक्तशुद्धि और कर्मकांड से नि:सृत होती थी; यह सिवाय एक मिथक के कुछ
नहीं है; इस मिथक की जड़ें औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञानकांड के लिए
‘नेटिव इंफार्मेंट’ का काम करने वाले, औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञानकांड से
अपने संपर्कों का लाभ उठाने वाले ब्राह्मण देवताओं की चतुराई में हैं। यह
उन असत्यों में सबसे प्रमुख है, जो सहज सत्य मान लिए गए हैं, और जो कबीर की
भक्ति के वास्तविक सामाजिक आशय तक पहुंचने में बाधक हैं।
भारतेन्दु हरिश्चंद्र के प्रहसनों— ‘सबै जाति गोपाल
की’ और ‘ज्ञाति विवेकिनी सभा’— से ज्ञात होता है कि पर्याप्त दक्षिणा लेकर
“निम्न” जातियों को चार वर्णों की व्यवस्था में उच्च और “उच्च” जातियों को
निम्न ठहराना देना ब्राह्मणों के लिए बांए हाथ का खेल है। असल में इस
खेल से जाति और वर्ण का पारंपरिक रूप से लोकमान्य संबंध ध्वनित होता है।
ताकतवर जातियां “उच्च वर्ण” से संबद्ध या उत्पन्न मान ली जातीं थीं। ‘अर्थ’
या ‘दंड’ के बल पर हासिल की गयी वास्तविक हैसियत को “शास्त्रवचन” की “उचित”
व्याख्या कर सैद्धांतिक धरातल पर भी “सिद्ध” कर दिया जाता था। जाति और वर्ण
का यह अंतस्संबंध भारतेन्दु के समकालीन अनुभव का भी
हिस्सा था। ‘सबै जाति गोपाल की’ में ‘पंडितजी’ ढूसरों को भृगुवंशी ब्राह्मण
सिद्ध करने के लिए “ज्वालाप्रसाद पंडित के शास्त्रार्थ” का हवाला देते हैं।[ix]
एक ज्वालाप्रसाद पंडित मुरादाबाद में भी थे।
इन्होंने उन्नीसवीं सदी में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और वर्ण-व्यवस्था
में उनके स्टेटस की विवेचना करने के लिए ‘जातिभास्कर’ ग्रंथ की रचना की थी।
इसमें वे अहीर और भील ब्राह्मणों, कोरई और खेचर क्षत्रियों का उल्लेख करते
हैं।
वर्ण-व्यवस्था में जातियों की हैसियत उठती गिरती रहती
थी। तुलसीदास की फैंटेसी “बरनाश्रम धरम निरत सब नर नारी” भारतीय इतिहास के
किसी भी काल की वास्तविकता नहीं मानी जा सकती। तुलसीदास के अपने समय में,
अकबर से परास्त होने वाला, दिल्ली का अंतिम हिन्दू राजा हेमू क्षत्रिय
नहीं, बक्काल (बनिया) था। ‘जाति-भास्कर’ के अनुसार सम्राट
हर्षवर्धन भी वैश्य कुल के ही थे।
इन सब बातों की उपेक्षा करते हुए, उपनिवेशवाद के “
ऑफिशियल ब्राह्मणों” की करतूतों को पारंपरिक सोच माना जाता है, यह
औपनिवेशिक सत्ता और उसके सहयोगियों की सफलता का प्रमाण है, लेकिन औपनिवेशिक
निर्मिति (कंस्ट्रक्ट) को परंपरा के ‘प्रामाणिक’ पाठ का दर्जा हासिल करने
में समय तो लगा ही। जिस दौर में ब्राह्मण लोग फोर्ट विलियम के साहबों को
यकीन दिला रहे थे कि उनकी जाति केवल कर्मकांडपरक संदर्भ में नहीं, बल्कि
सामाजिक व्यवहार मात्र में सर्वोच्च मानी जाती है, जिस समय सेंसस कमिश्नर
रिज्ले साहब रक्त शुद्धि का निर्धारण करने के लिए इंची टेप से लोगों
की नाकें नाप रहे थे; उसी समय मारवाड़ रियासत की ‘मर्दुमशुमारी’ (1891) के
आधार पर मारवाड़ रियासत के पचीस लाख बाशिंदों की “रीत-भांति और चाल-चलगत के
हालात” लिखने वाले मुंशी हरदियाल सिंह की रिपोर्ट (1896) सामाजिक पदानुक्रम
को वास्तविक जीवन-व्यवहार के आधार पर बखानने की पद्धति अपना रही
थी।
इस मनोरंजक और विचारोत्तेजक प्रसंग की चर्चा हम
अगले अध्याय में करेंगे।
औपनिवेशक सत्ता ने अपनी ज़रूरतों के कारण और
ओरिएंटलिस्ट विद्वानों ने अपने संस्कारों के कारण माना और मनवाया कि
उनके श्रीचरण पड़ने के ऐन पहले का भारतीय समाज अपनी बौद्धिक चमक कब की पीछे
छोड़ आया था। देशभाषाएं तो भोले-भाले, गंवारों की ही भाषाएं थीं। बौद्धिक
रूप से, जो कुछ काम का था( अगर था तो!), वह या तो संस्कृत में था, या फिर
फारसी में। स्वर्ण-युग (अगर था तो!) कब का बीत चुका था। “मध्यकाल” क्या
साहित्य में, क्या चिंतन में बस अनुवाद और अनुगमन करने लायक ही रह गया था।
और ऐसे जबदे हुए काल का “इमीडिएट सक्सेसर” होने के नाते 18वीं-19वीं सदी के
भारत के भाग्य में यही बदा था कि अब वह अपने आप को पहचानने तक के
लिए18वीं-19वीं सदी में यूरोप द्वारा रचे जा रहे “ज्ञान” और
“भारतविद्या” का अनुगमन करे।
कबीर के ही नहीं, अन्य प्रसंगों में भी, बहुत से सहज
स्वीकार्य मान लिए गए प्रस्थान और निष्कर्ष ऐसे ही अनुगमन के परिणाम हैं।
नाना प्रकार के वैचारिक गोत्रों से संबद्ध ज्ञानीजन-मुनिगण सारे परस्पर
मतभेदों के बावजूद कबीर के समय के बारे में ऐसी अनेक बातों को
निर्विवादत: स्वयंसिद्ध मान लेते हैं, जिनकी “खोज” ही नहीं “रचना” भी
औपनिवेशिक सत्ता की आवश्यकताओं के मुताबिक की गयी है। जो सामाजिक संस्थाएँ,
परंपराएँ और आदतें औपनिवेशिक काल में विकसित हुईं, (कई बार तो औपनिवेशिक
सत्ता द्बारा जान-बूझ रची गयीं), या भारत के किसी एक क्षेत्र तक सीमित थीं,
उन्हें औपनिवेशिक ज्ञानकांड और थ्योरी ने भारतीय समाज की “शाश्वत और
अखिल-भारतीय विशेषताएँ” “सिद्ध” कर दिया।
यह औपनिवेशिक सार्वत्रिकता भी लोक-जीवन के दैनंदिन
व्यवहारों से उतनी ही दूर थी, जितनी कि स्मार्त्त सार्वत्रिकता। स्थानीय
रीत-भाँत और समुदायों तथा बिरादरियों के विशिष्ट रिवाजों के प्रति इसमें भी
वैसी ही अवहेलना थी, जैसी कि स्मार्त्त परंपरा में। औपनिवेशिक सत्ता के साथ
ब्राह्मणों की जुगलबंदी स्वाभाविक ही थी।
गाँधीजी जब इंग्लैंड से बैरिस्टर बन कर लौटे तो
उन्हें ‘परंपरा का पालन करते हुए’, समुद्र पार करने के पाप का प्रायश्चित
करना पड़ा था। उन्होंने नासिक में गोदावरी स्नान तो कर लिया, लेकिन बिरादरी
भोज देने से इंकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बहन की और खुद गांधीजी की
ससुराल में उन्हें ‘अपवित्र’ ही माना जाता रहा।[x]
यह ‘परंपरा-पालन’ 1891में हुआ था।
दो सदी पहले गुजराती व्यापारी लगातार समुद्र पार करते
रहते थे। उनके कारोबार अरब और अफ्रीका तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक व्यापारी
थे—मेहराज ठाकुर( 1618-1694)। इतिहास के अध्येता इन्हें प्रणामी संप्रदाय
के संस्थापक, महामति प्राणनाथ के रूप में बेहतर जानते हैं। 1668 में अरब
डाकुओं ने इनकी पत्नी तेजकुंवरि का अपहरण कर लिया था। वे अरब जाकर
डाकुओं को फिरौती देकर पत्नी को छुड़ा लाए,कोई प्रायश्चित उन्हें नहीं करना
पड़ा। तेजकुंवरि को महामति प्राणनाथ ने अपवित्र मानकर त्याग नहीं
दिया, उनके साथ सहज रूप से जीवन-यापन करते रहे।[xi]
दो सौ सालों में गुजरात के व्यापारियों के परंपरा-बोध
में ऐसा जबर्दस्त परिवर्तन लाने में कुछ समुदायों और क्षेत्रों तक सीमित
समुद्र-यात्रा-निषेध को सारी हिन्दू परंपरा की अखिल-भारतीय, सार्वत्रिक
विशेषता बताने वाले औपनिवेशिक ज्ञानकांड और उसके सहयोगियों की कुछ भूमिका
रही होगी या नहीं?
औपनिवेशिक ज्ञानकांड का जन्म यूरोपीय आधुनिकता से हुआ
था। यूरोपीय आधुनिकता के प्रस्थानों और ‘स्वयंसिद्धों” की कड़ी आलोचना
उत्तर-आधुनिकता ने की है। किन्तु, भारतीय समाज के प्रसंग में
उत्तर-आधुनिकता के अधिकांश अलम-बरदार यूरो-केन्द्रित आधुनिकता से भी बदतर
साबित हुए हैं। ये लोग भारतीय राष्ट्रवाद का ‘विखंडन’- डिकंस्ट्रक्शन तो जम
कर रहे हैं, लेकिन औपनिवेशिक ज्ञानकांड का विखंडन इनकी प्राथमिकताओं
में कहीं नहीं दिखता।
देशभाषा स्रोतों में अंतर्निहित लोक-चेतना को
गंभीरता से लिए बिना, सारी की सारी परंपरा को साजिश मानने की बीमारी से
पिंड छुड़ाए बिना भारतीय, या किसी भी परंपरा के आत्मसंघर्ष को समझना असंभव
है। उपनिवेशवाद की दूरगामी सांस्कृतिक निष्पत्तियों को समझे बिना
ब्राह्मणवाद का सार्थक खंडन भी असंभव है। मन में जिज्ञासा यह भी है कि
ब्राह्मणवाद के तीक्ष्ण खंडन और सांस्कृतिक अस्मितावाद के मुखर मंडन के इस
दौर में, एक तरफ सामाजिक वर्गों की अवधारणा का, और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद के
प्रभावों के प्रश्न का, विमर्श के हाशिए पर पहुंच जाना मात्र संयोग
है क्या? इसके पीछे नव-साम्राज्यवाद की कोई रणनीति, कोई ‘पावर-पॉलिटिक्स’
है या नहीं?
ये तथा ऐसी अन्य जिज्ञासाएं लेकर चलते-चलते कई बरस
गुजर गए। इस यात्रा की रिपोर्टें बीच-बीच में प्रस्तुत करता रहा। यह किताब
भी इस जिज्ञासा-यात्रा की रिपोर्ट ही है। इस बार तनिक विस्तार के साथ।
कबीर के साथ मेरा नाता जिज्ञासा का, सतत यात्रा का
नाता है।
4.मानवीय चैतन्य का साझा
सपना.
कबीर की कविता इस जिज्ञासा-यात्रा में कदम-कदम पर याद
दिलाती रही हैः अनंत अस्तित्व से संबंद्ध होने का विस्मय, उल्लास और संताप
उतना ही प्रामाणिक है, जितना कि सामाजिक अन्याय के प्रति रोष। मनुष्य का
सहज बोध, मार्क्स के शब्द याद करें तो-मनुष्य का “प्रजाति सार” ( स्पेसि
एसेंस)- अनंत ब्रह्माण्ड से जुड़ाव के सुख-दु:ख और समाज के सुख-दु:ख का वहन
एक साथ करता है। मनुष्य की आत्मपरिभाषा है यह बोध। मनुष्य मनुष्य है ही इस
वजह से कि वह प्रकृति का केवल अंग नहीं, आत्मचेतस अंश है। वह अस्तित्व के
साथ अपने संबंध के बारे में सचेत है। फिर से मार्क्स के शब्दों तक चलें, तो
मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध ‘ऑर्गेनिक’ न होकर ‘इन-ऑर्गेनिक’ है।
‘स्प्रिचुअल’ है। यहाँ ‘स्प्रिचुअल’ शब्द मार्क्स का ही है, मेरा नहीं।[xii]
बार-बार याद दिलाती है कबीर की कविता :
लौकिक-अलौकिक, भीतर-बाहर, सामाजिक-आध्यात्मिक में विरोध नहीं
है। अविरोध के इस बोध को खोजने कहीं ‘बाहर’ नहीं जाना पड़ता। अपने ऊपर थोप
लिए गए अधूरेपन से यदि मुक्ति पा सकें, पूरेपन के मनमाने टुकड़े करने की
आदत से यदि पिंड छुड़ा सकें, तो हम अपने “घट-भीतर” के इस अहसास के प्रति,
अपने ‘स्पेसि-एसेंस’ के प्रति फिर से सचेत हो सकते हैं:
खोजी होय तो तुरतै मिलि हौं पल भर की तलास में
कहै कबीर, सुनो भई साधो, सब स्वाँसों की स्वाँस में।
लौकिक-अलौकिक, भीतर-बाहर, सामाजिक- आध्यात्मिक की
निरंतरता; और परस्पर निर्भरता के ‘बाहर-भीतर सबद निरंतर’ को लगातार सुनते
रहने को, इस के अनुकूल जीवन जीने को ही कबीर “घट-साधना” कहते हैं। मूलभूत
प्रश्न— जो कई रूपों में उनकी कविता में आता है— यही है कि प्रेम से यदि
परमात्मा मिल सकता है, भक्ति यदि राम को रिझा सकती है, तो सामाजिक व्यवहार
में प्रेम और भक्ति पर जाति,मजहब और कुल क्यों भारी पड़ते हैं? उनकी
बहुचर्चित और बहुप्रशंसित सामाजिक चेतना और तज्जनित सामाजिक आलोचना कबीर की
आध्यात्मिक खोज की ही परिणति है। कबीर के “क्रांतिकारी” प्रशंसकों को जो
‘घट-साधना’ उलझन में डालती है, उसके बिना कबीर की सामाजिक चेतना और आलोचना
संभव ही नहीं थी। कबीर समाज को देखते ही उस सपने की आँखों से हैं, जो उनकी
घट-साधना उन्हें दिखाती है।
इस सपने की आँखों से दुनिया देखते कबीर अपनी सामाजिक
पहचान से नहीं कतराते। जाति के सवाल पर उस तरह चिढ़ने नहीं लगते, जैसेकि
‘कवितावली’ में तुलसीदास चिढ़ उठते हैं कि उन्हें किसी की बेटी से अपना
बेटा ब्याह कर उसकी जाति नहीं बिगाड़नी है (कवितावली, उत्तरकांड, छंद,
106)। इस चिढ़ में ‘पोयटिक जस्टिस’ है। ‘कवितावली’ के तुलसी जिस जिज्ञासा
से इतने चिढ़ते हैं, वह ‘मानस’ के तुलसी के मतानुकूल है। उन्हीं ने तो
स्वयं राम के मुख से कहलाया था,‘पूजिए विप्र गुण-गन-ज्ञानहीना,
पूजिए न सूद्र सकल गुन प्रबीना!’ ‘रामचरितमानस’ का रचयिता यदि कोई शूद्र
होता तो उसे “पूज्य” मानने में स्वयं तुलसी को कितनी दिक्कत होती! तुलसी से
उनकी जाति पूछ कर उन्हें संतप्त करने वाले, असल में स्वयं तुलसी के कहे
मुताबिक ही चल रहे थे। विडंबना यह थी कि बात जब खुद पर आ पड़ी तो तुलसीदास
चिढ़ने लगे।
कबीर अपनी जाति से क्यों भागें? वे जन्मजात पूज्यता
का दावा भी क्यों करें? उनमें आत्मविश्वास है, अनभय, अनुभव और रहनि का,
पूज्यता की परवाह किए बिना, मरजीवा बन कर जीने का । स्वयं को ‘जात जुलाहा,
मति का धीर’ कहने का। वे विडंबनापूर्ण ढंग से कह सकते हैं : ‘आइ हमारे कहा
करोगी, हम तो जात कमीना’। पूज्यता प्राप्त करने में कबीर की अपनी कोई रुचि
नहीं थी। वह तो अपने एकांत में बाधा डालने वाली, व्यर्थ की लोकप्रियता को
दूर भगाने के लिए कौतुक तक कर बैठते थे। ऐसे कौतुक का विवरण अनंतदास ने
दिया है। यह और बात है कि पूज्यता के प्रति कबीर की अरुचि के बावजूद
कबीर के समाज ने उन्हें पूजा और खूब पूजा। आज तक पूज रहा है।
अपनी जाति से भागने की बजाय कबीर वर्ण-व्यवस्था के
मूल तर्क पर प्रहार करते हैं। वे जानते हैं कि जन्मजात पूज्यता और अपूज्यता
को सिरे से खारिज़ किए बिना न वास्तविक नैतिकता की प्रतिष्ठा संभव है, न
उत्तरदायी व्यक्तित्व की। कबीर जाति पर आधारित सम्मान-असम्मान की धारणा को
समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरह के जातिवाद को हटा कर दूसरी तरह
के जातिवाद को पधरा देने की नहीं। उनके हिसाब से, किसी को शूद्र होने
भर के कारण ‘नीच’ मानना निचाट मूर्खता है, और उतनी ही निचाट मूर्खता
है,किसी को ब्राह्मण होने मात्र के कारण दुष्ट मानना।
“जुलाहे का दुख केवल जुलाहा ही समझ सकता है”, यह
आजकल का ज्ञान है। जाति के जुलाहे और मति के धीर कबीर का ज्ञान जुदा किस्म
का था। वे जानते थे कि सिर्फ अपना और अपने जैसों का ही नहीं, बल्कि अन्यों
का भी दुख समझने की कोशिश किए बिना, परकाया-प्रवेश की साधना किए बिना कविता
न लिखी जा सकती है, न सुनी जा सकती है। कबीर को केवल जुलाहा, शूद्र या दलित
होकर ही समझा जा सकता है—यह कहना कबीर की संप्रेषण-क्षमता को, उनके कवित्व
को सिरे से नकारना है।
कबीर कहीं यह नहीं कहते कि ‘कहे कबीर सुनो भई
जुलाहो’! उनके कुछ संबोध्य श्रोता -‘पांडे’, मौलाना’ या ‘जोगी’—कबीर के
व्यंग्यों के लक्ष्य हैं। जिस श्रोता से वे दोस्ताना लहजे में बात करते
हैं, कबीर का वह श्रोता ‘साधु’ है ‘भाई’ है, जातभाई नहीं।
मनुष्य की अनिवार्य और निरंतर पहचान उसकी मनुष्यता
ही है। इस पहचान के साथ ही वह विविध सामाजिक पहचानों को धारण करता है।
जाति, धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता—किसी एक पहचान को ही एकमात्र सामाजिक पहचान
मान लेना सामाजिक अस्मिता का फंडामेंटलिज्म है,और हर फंडामेंटलिज्म की तरह
फंडामेंटली खतरनाक है। किसी भी फंडामेंटलिज्म की तरह इसकी भी यात्रा
फ़ासिज्म की ओर ही है।
कबीर की कविता की ताकत इस जिद में है कि वे कविता कर
रहे हैं, ऐसे जगत में जहाँ बहुत से लोग साधु का ज्ञान नहीं, उसकी जाति
पूछते हैं, लेकिन सपना देखते हैं, ऐसे समय का, ऐसे अमरदेस का जहाँ मनुष्य
का मोल,उसकी जाति के आधार पर नहीं, साधना के आधार पर होगा। ऐसे समाज का,
जिसके आधारभूत नैतिक प्रतिमान सार्वभौम और सार्वजनीन होंगे। उनका सपना किसी
एक जाति, बिरादरी, पंथ या मजहब का सपना नहीं, मनुष्य के साझे चैतन्य का
सपना है। वह ‘नया पंथ निकालने’ का नहीं, धर्म के ‘फाउस्टियन पैक्ट’ से
मनुष्य की मुक्ति का, धर्मेतर अध्यात्म का सपना है।
यह अकेले कबीर का नहीं, मानवीय चैतन्य मात्र का साझा
सपना है। देशभाषाओं की सहस्राब्दी में, भारत समेत अनेक समाज इस सपने की ओर
यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा में यूरोप और गैर-यूरोप में बहुत कुछ साझा था,
और बहुत कुछ विशिष्ट भी। इक्कीसवीं सदी में मानव के साझे चैतन्य पर आधारित,
न्याय-चेतना पर आधारित दुनिया बनाने के लिए ऐसे साझेपन और वैशिष्ट्य दोनों
का बोध आवश्यक है। इसी तरह, कबीर की संवेदना के साथ अध्येता की अपनी
संवेदना के साझेपन और अलगपन दोनों के प्रति सचेत रहना जरूरी है। ऐसी चेतना
का कबीर से नाता इस्तेमाल या अंधानुगमन का नहीं, मानवीय सपनों के परस्पर
संवाद का नाता होगा।
मानवीय सपनों से जुड़ी है, मानवाधिकारों की बात। आजकल
यही माना जाता है कि दूसरी बहुत सी चीजों की तरह मानवाधिकारों की
धारणा का विकास भी यूरोप के बाहर भला कहां हो सकता था। ध्यान रखना चाहिए कि
यह तो सही है कि मानवाधिकार की धारणा ठेठ आधुनिक धारणा है, लेकिन यह कतई
सही नहीं कि आधुनिकता ठेठ यूरोपीय धारणा है।
निर्गुण भक्ति-संवेदना के साथ यदि गंभीर संवाद करे
तो, मानवाधिकारों का समकालीन विमर्श न केवल समृद्धतर हो सकेगा,
बल्कि उसे अपने उन पुरखों का पता भी चल सकेगा, जो यूरोप के बाहर जन्मे थे।
वर्णाश्रम, भक्ति-संवेदना और मानवाधिकार की चर्चा
इस पुस्तक में आगे करेंगे।
5. ‘जन कबीर का सिखरि घर’:
फैंटेसी, यूटोपिया और धर्मेतर अध्यात्म.
भक्त कवि फैंटेसी और यूटोपिया के कवि हैं। वे
निर्गुण या सगुण राम या श्याम से नितांत निजी रिश्ते की फैंटेसी रचते हैं।
वास्तविक जीवन में जो अकेलापन उसकी नियति है, जिसमें ऐसा कोई मिलना मुश्किल
हो गया है, जिससे अपने मन की बात ‘नि:शंक’ भाव से कही जा सके; उस अकेलेपन
के समानांतर भक्त रचता है, अपने प्रभु, सखा, बालम के संग- साथ निरंतर चलने
वाले प्रेमालाप की फैंटेसी। ‘प्रिय’ को रिझा कर आँख की पुतली में मूँद लेने
की निजी फैंटेसी के साथ, वह एक कल्पना-लोक भी रचता है, वैयक्तिक और सामाजिक
यथार्थ के समानांतर एक यूटोपिया।
भक्तों के यूटोपिया वस्तुत: जन-साधारण के ही यूटोपिया
हैं। ‘अमरदेश’, ‘बेगमपुर’, ‘सिंहल-द्वीप’ या ‘रामराज्य’ लोक-कल्पना में
निहित आकांक्षाओं से ही आते हैं। लोक-कथाओं में न जाने कितने
राजकुमार गए होंगे, सिंहल द्वीप की राजकुमारी को ब्याह लाने के लिए। यही
सिंहल द्वीप जायसी के ‘पद्मावत’ में जायसी का अपना कवि-सपना बन कर आता है।
तुलसीदास का ‘रामराज्य’ भी इसी तरह, लोक-जीवन से आया हुआ सपना है, जिसे
तुलसीदास अपने वर्णाश्रमवादी दुराग्रहों के कारण,दु:स्वप्न में बदल देते
हैं—और मर्मस्पर्शी रामकथा के अधिकांश को नीरस उपदेश में।
कबीर और दूसरे निर्गुण संतों के स्वप्न ‘बरनाश्रम धरम
निरत सब नर-नारी’ से पहचाने जाने वाले तुलसीदासीय ‘रामराज्य’ से एकदम
विपरीत प्रकार के हैं। इन स्वप्नों से बहुत से लोग प्रेरणा लेते रहे हैं,
तो कुछ लोग उन्हें विकृत भी करते रहे हैं। निर्गुण संतों के स्वप्नों के
स्रोतों, परिणतियों और विकृतीकरणों का अध्ययन भक्ति संवेदना के ही नहीं,
भारत के सामाजिक इतिहास के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण बातें बताएगा। मेरे
कुछ जिज्ञासु मित्र विभिन्न संतों के संदर्भ में ऐसा अध्ययन कर भी रहे हैं।
कबीर की कविता सपना देखती है, ऐसे अमरलोक का, जिसमें
मनुष्य की मनुष्यता ही महत्वपूर्ण है। कबीर के देखे सपने में न ब्राह्मण
है, न क्षत्रिय। न सैयद है, न शेख। न शूद्र है,न वैश्य। कबीर का सपना न तो
सिर्फ सामाजिक ‘मुक्ति’ तक सीमित है, न सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति तक। उनके
सपने में ये दोनों मुक्तियां एक दूसरी का विरोध नहीं, पोषण करती हैं।
कबीर की बानी में यह सपना आने वाले वक्त
की कल्पना से कहीं अधिक, पीछे छूट गए घर की स्मृति का रूप ले कर आता है। वह
यूटोपिया कम, नॉस्टेल्जिया ज़्यादा है। उस वक्त का नॉस्टेल्जिया, जब मनुष्य
को मनुष्य बनाने वाली उसकी विशेषता, उसके “प्रजाति-सार”, उसकी
अध्यात्म-सत्ता का अपहरण धर्म-सत्ता द्वारा नहीं हुआ था। संगठित धर्म-मतों
के उदय के पहले की वह अध्यात्म-सत्ता एक आदिम स्मृति और एक संभावना
के रूप में हमारी चेतना के आकाश में अभी भी कौंधती है। इसी कौंध को कबीर
“अमरपुर” कहते हैं, उस अमरपुर से ही वे आए हैं, वहीं जाना चाहते हैं।
यूटोपिया को नॉस्टेल्जिया बना कर कबीर की कविता अपने
आत्मविश्वास को रेखांकित करती है। ‘अमरदेश’ वर्तमान देशकाल में नजर भले न
आए; स्मृति और कल्पना में, मौजूद है। आने वाले कल की कल्पना बीत चुके कल
की वेदना बन जाती है। स्मृति और कल्पना के इस अनपेक्षित संबंध से कबीर की
कविता को अद्भुत मार्मिकता मिलती है। उनकी कविता में बारंबार आने वाले घर
और पीहर कल्पना और स्मृति के इस संबंध के रूपक हैं। कविता में नारी रूप
धारते कबीर को सताने वाली पीहर की याद यूटोपिया और नॉस्टेल्जिया के
वेदनापूर्ण संयोग को हमारे सामने मूर्त कर देती है।
पं0 सर्वजीत को छकाती, उन्हें यह बताती कमाली कि कबीर
का घर ऐसे शिखर पर है, जहां चींटी तक के पाँव फिसलते हैं—कबीर की
कल्पना और स्मृति के विस्तार का ही संकेत कर रही थी। स्मृति व्यक्तिगत भर
नहीं, किसी एक सांस्कृतिक परंपरा तक सीमित भर भी नहीं, मनुष्य-मात्र
की चेतना में बद्धमूल स्मृति । मनुष्य के ‘प्रजाति-सार’ की स्मृति । कबीर
का ‘घर’- अमरलोक— स्मृति और कल्पना के जिस संयोग का रूपक है उसमें
सामाजिक सरोकार और आध्यात्मिक आकांक्षा एक-दूसरे को काटते नहीं। अपने घर
की याद और अमरपुर की कल्पना में कबीर जिन ‘डॉयकाटॉमीज़’- जिन द्विभाजनों-
के परे जाते हैं, उन्हीं के सामाजिक, संस्थाबद्ध रूपों से कविता में लोहा
लेते हैं।
यों तो सभी परमपिता परमात्मा की संतान या फिर
सर्वव्यापी ब्रह्म के विविध रूप ही हैं, लेकिन फिर भी, कोई जन्म से ही
‘नीच’ है, और कोई जन्म से ही ‘पूज्य’। कोई पैगंबर विशेष पर ईमान लाने के
कारण ही ‘पवित्र’ हो गया है, और कोई महज़ उस पैगंबर को कबूल न करने के कारण
ही ‘अपवित्र’ रह गया है। मानुष-सत्य को इस तरह बाँटने और काटने वाले
सामाजिक सत्ता-तंत्रों और उसकी चतुर रणनीतियों, पाखंडों से कबीर की चिढ़
जगजाहिर है। ऐसी रणनीति के हरेक रूप को कबीर रद्द करते हैं- उसे चाहे वेद
के हवाले से प्रस्तुत किया जाए, चाहे क़ुरान के हवाले से।
कबीर ने कहा, ‘तुम जिन जानो यह गीत है, यह तो निज
ब्रह्म विचार रे’। बाद में, उनके नाम से पंथ चला दिया गया। फलस्वरूप बीसवीं
सदी के अध्येताओं में कबीर को “धर्मगुरु” कहने की चाल चल पड़ी।
कोई कहते हैं कि कबीर ने ‘अपना निराला पंथ निकाला’; तो किसी के हिसाब से वे
हिन्दू-मुस्लिम धर्मों की आलोचना कर ही इसलिए रहे थे कि अपने नए धर्म के
लिए जगह बना सकें। किसी के अनुसार, कबीर को इस्लाम की आलोचना से कोई मतलब
ही नहीं था, वे तो केवल हिन्दू धर्म को ध्वस्त कर रहे थे, ताकि मक्खलि
गोशाल के आजीवकवाद का दलित धर्म के रूप में पुनराविष्कार कर सकें।
सभी धर्ममतों के आलोचक कबीर को धर्मप्रवर्तन के लिए
उत्सुक धर्मगुरु मानने का संबंध आधुनिक, उत्तर-आधुनिक अहंकार से है। यों
चलता है अहंकारी तर्क : धर्मसत्ता मात्र के नकार का साहस और बौद्धिक
प्रयत्न हम आधुनिक और उत्तर-आधुनिक होकर भी नहीं जुटा पाते, तो उस “पिछड़े”
वक्त में, वह भी गैर-यूरोपीय परिवेश में धर्मसत्ता के हर रूप को
खारिज करने की बात कोई सोच भी कैसे सकता था? जब हमें आदत है- या तो धर्म के
साथ अध्यात्म को भी खारिज कर देने की, या फिर अध्यात्म पर धर्म का ही
एकाधिकार मान लेने की-तो कबीर जैसे “अनपढ़” भला कल्पना तक कैसे कर सकते थे,
धर्मेतर अध्यात्म की?
विनम्र भाव से कबीर तक जाने वाले देख सकेंगे कि उनकी
महत्वाकांक्षा धर्मप्रवर्तक बनने से कहीं ऊंचे दर्जे की थी। वे मनुष्य के
“प्रजाति सार” को एक धर्मसत्ता की जकड़ से छुड़ाकर दूसरी के हवाले नहीं कर
देना चाहते थे। वे ब्रम्हाण्ड के साथ मनुष्य के “स्प्रिचुअल” रिश्ते को
धर्म द्वारा पैदा किए गए वस्तूकरण-“रीइफिकेशन”- की जकड़ से मुक्त करने का,
धर्मेतर अध्यात्म का सपना देखते थे। कबीर के अमरलोक की एक विशेषता यह
भी है कि “ धरम करम कछु नाहीं उंहंवा, ना उहां वेद विचारा”। इस बारे में
चर्चा कबीर की साधना के प्रसंग में करेंगे।
कबीर के अमरलोक में साधारण मनुष्य
विराट से साक्षात्कार के असाधारण अनुभव से गुजरता है। कबीर की कविता हमें
अवसर देती है कि हम अपनी सीमित मनुष्य-सत्ता के साथ ही असीम ब्रह्मांड से
सबद्धता की झलक पा सकें। इसी झलक के विस्मय को आइंस्टीन ने ‘कॉस्मिक
वंडर’ कहा था। कबीर का अनुभव इस ‘कॉस्मिक वंडर’—विराट विस्मय—के निजी
उल्लास और वेदना को व्यंजित करता है:
हम बासी उस देस के जहाँ बारह मास विलास।
प्रेम झरै विकसै कँवल तेज
पुंज परकास।
हम बासी उस देस के जहाँ जाति बरन कुल नाहिं।
सबद मिलावा होय रहा देह मिलावा नाहिं।
[i]
विलियम क्रुक, ‘
दि ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया’
( पुनर्मुद्रण, कॉस्मो पब्लिकेशंस, दिल्ली, 1975), खंड-तीन, पृ074.
[ii]
पीतांबरदत्त बड़थ्वाल,
‘योग-प्रवाह’
( श्री काशी विद्यापीठ, बनारस, 1945), पृ0 203-204.
[iii]
शैल्डॉन पोलक, ‘दि
लैंगवेज़ ऑफ गॉड्स इन दि वर्ल्ड ऑफ मेनः संस्कृत,कल्चर ऐंड पॉवर इन
प्रि-मॉ़डर्न इंडिया’
( परमानेंट ब्लैक, नयी दिल्ली, 2007),पृ0507.
[iv]
इमेनुएल वार्लस्टाइन, ‘दि
एंड ऑफ दि वर्ल्ड ऐज वी नो इटः सोशल साइंस फॉर दि ट्वेंटी-फर्स्ट
सेंचुरी’,
( यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा प्रेस, लंदन, 1999), पृ0 1.
[v]
निकोलस डर्क्स, ‘
कास्ट्स ऑफ माइंड: कॉलोनियलिज्म ऐंड दि मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया’,
परमानेंट ब्लैक, दिल्ली, 2002,पृ0 222.
[vi]
आशुतोषदयाल माथुर,
‘ मीडिएवल हिन्दू ल़ॉः
हिस्टॉरिकल इवोल्यूशन ऐंड एनलाइटेंड रिबेलियन’
(ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली 2007), पृ01.
[vii]
रामचंद्र शुक्ल,
‘हिन्दी साहित्य का
इतिहास’ (
संस्करण सं0 2035 वि0), नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ091.
[viii]
विलियम क्रुक, ‘
दि ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया’
– खंड तीन, 1896,(
पुनर्मुद्रण, कॉस्मो पब्लिकेशंस,नयी दिल्ली, 1975), पृ0
CIXIX.
[ix]
‘भारतेन्दु समग्र’
(सं0 हेमन्त शर्मा, हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी,
1989), पृ0543.
[x]
राजमोहन गाँधी,
‘मोहनदासः ए ट्रू
स्टोरी ऑफ ए मैन, हिज पीपुल ऐंड एन एंपायर’
( पेंग्विन वाइकिंग, नयी दिल्ली, 2006), पृ054.
[xi]
रणजीत साहा, ‘
महामति प्राणनाथ’
( साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, 2003), पृ0 10.
[xii]
बहुत विचारोत्तेजक है,
कार्ल मार्क्स की विस्मृतप्राय रचना ‘इकानॉमिक
ऐंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स-1844’
से गुजरना। कुछ विस्तृत चर्चा के लिए देखें, दैनिक
‘जनसत्ता’
में ‘मुखामुखम’
स्तंभ के रूप में प्रकाशित मेरे लेखों का संकलन—
‘निज
ब्रह्म विचार’, ,(
राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली 2004.)
[xiii] “यह
पद प्रक्षिप्त है, बीजक में नहीं पाया जाता। यह किसी चतुर ब्राह्मण की
करतूत है”।–
डॉ0बच्चनसिंह, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, (राधाकृष्ण
प्रकाशन, नयी दिल्ली,
1996), पृ091.
[xiv]
डॉ0 रामकुमार वर्मा,
संत कबीर’(
साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1966), पृ0 51-52.
[xv]
देखें विनांद कैल्वर्त्त,
दि सर्वंगी ऑफ गोपालदास, मनोहर, नयी दिल्ली, 1993, पृ0261.
[xvi]
रामचरितमानस, उत्तरकांड,
दोहा 97 से 99 तक. गीताप्रेस, गोरखपुर गुटका संस्करण( सं0 2030) में
पृ0 651 और 653.
[xvii] ‘राम’
की अवधारणा पर भक्ति-विमर्श के भीतर चले विवाद के सांस्कृतिक, वैचारिक
आशयों की पड़ताल के लिए देखें मेरा लेख- ‘सांस्कृतिक
बहस का एक रूपकः कण-कण में व्यापे हैं राम’
(पुरुषोत्तम अग्रवाल ‘संस्कृतिःवर्चस्व
और प्रतिरोध’,
राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2008-दूसरा संस्करण), पृ0 138-157
[xviii]
‘पब्लिक स्फीयर’
के लिए ‘लोकवृत्त’
शब्द के उपयोग के औचित्य के बारे में देखें मेरा लेख, ‘लोकवृत्त:
हिन्दी भाषा या हिन्दी प्रदेश का?’
‘आलोचना’सहस्राब्दी
अंक 15, सं. नामवरसिंह, राजकमल, नयी दिल्ली, अक्टूबर-दिसंबर, 2003, पृ0
113-125.
[xix]
डॉ0 रामविलास शर्मा, ‘भारतीय
साहित्य की भूमि्का’,
( राजकमल, ( नयी दिल्ली, 1996), पृ0120.
[xx] ‘गोरखबानी’,
(सं0 डॉ. पीतांबरदत्त
बड़थ्वाल), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1942, पृ0 91, 94 और 104.
[xxi] ‘कबीर
ग्रंथावली’, (सं0
डॉ. माताप्रसाद गुप्त, साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1985, पृ0 117, 285 और
372.
[xxii]
आनंद कुमारस्वामी,
‘हिन्दूइज्म ऐंड
बुद्धिज्म’
मुंशीराम मनोहरलाल, नयी दिल्ली, संस्करण 2007, पृ0 20.
[xxiii]
यह टुकड़ा इतिहासकार
रंजीत गुहा का है। देखें उनका लेख, ‘डॉमिनेंस
विदाउट हेगेमनी ऐंड इट्स
हिस्टीरियोग्राफी’
( सब-आल्टर्न स्टडीज, खंड 6, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी
दिल्ली, 1989), पृ0259
[xxiv]
रामचंद्र शुक्ल, ‘गोस्वामी
तुलसीदास’ नागरी
प्रचारिणी सभा, काशी, सं0 2033, पृ0 16.
आगे
पढें

कहाँ कबीर कहाँ हम
अमीर
खुसरो
- जीवन कथा और कविताएं
जो कलि नाम कबीर न होते...’
जिज्ञासाएं और समस्याएं
कबीरः एक
समाजसुधारक कवि
कबीर की
भक्ति
नानक
बाणी
भक्तिकालीन
काव्य में होली
भ्रमर
गीतः सूरदास
मन
वारिधि की महामीन - मीरांबाई
मीरां का
भक्ति विभोर काव्य
मैं कैसे
निकसूं मोहन खेलै फाग
रसखान के
कृष्ण
रामायण की
प्रासंगिकता
सीतायाश्चरितं महत
सूर और
वात्सल्य रस
विश्व की
प्रथम रामलीला

|
|
|
Hindinest is a website for creative minds, who
prefer to express their views to Hindi speaking masses of India.
|
|