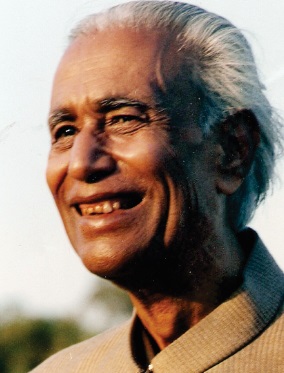घाट से लौटते हुए
तीसरे प्रहर की अलसायी बेला में
मैं ने अकसर तुम्हें कदम्ब के नीचे
चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया
मैं ने कोई अज्ञात वनदेवता समझ
कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया
पर तुम खड़े रहे‚ अडिग‚ निर्लिप्त‚ वीतराग‚ निश्चल!
तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं!
दिन पर दिन बीतते गए
और मैं ने तुम्हें प्रणाम करना तक छोड़ दिया
पर मुझे क्या मालूम था कि वह स्वीकृति ही
अटूट बंधन बन
मेरी प्रणाम–बद्ध अंजलियों में
कलाईयों में इस तरह लिपट जाऐगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी।
मुझे क्या मालूम था कि
तुम केवल निश्चल खड़े नहीं थे
तुम्हें मेरे प्रणाम की मुद्रा और मेरे
हाथों की गति इस तरह भा गई थी कि
तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति
को पूरी तरह बांधना चाहते थे।
इस सम्पूर्ण के लोभी तुम
भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते?
मुझ पगली को देखो‚
मैं समझती रही कि
तुम कितने वीतराग हो‚
कितने निर्लिप्त।
कविताएँ
एक कविता 'कनुप्रिया' से
आज का विचार
दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो।
आज का शब्द
दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो।