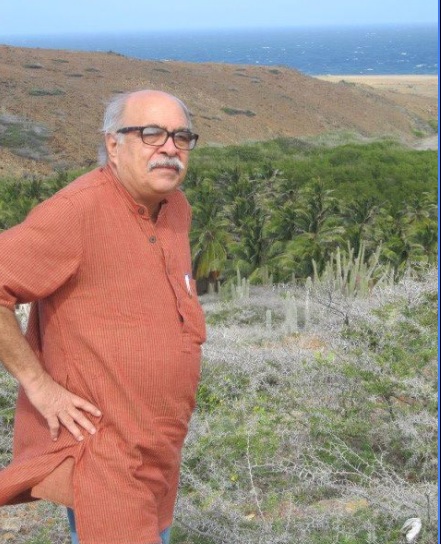– शायद आठवें दशक के मध्य का दौर रहा होगा। तब दिल्ली ‘महा गांवड़ा` की काया से मुक्त होकर महानगर काया की देहधारी बनी ही थी। कॉफी हाउस का नूर बऱकरार था। आज की तरह बहुराष्ट्रीय ‘झटपटिया भोज रेस्तरां` कनॉट प्लेस में कुकुरमुत्ते की भांति उगे नहीं थे। लिहाज़ा बौद्धिक महारथियों और किफायती जेबधारियों का यदि कोई ‘मक्क-काशी` हुआ करता था तो वह था इण्डियन कॉफी हाउस। बाबा खड़गसिंह मार्ग पर तैनात मोहन सिंह प्लेस बिल्डिंग के तीसरे तल पर आबाद यह कॉफी हाउस मुझ जैसे स्थूल प्रज्ञावान राजनीतिज़् पत्रकार के लिए भी शाम-ए-पनाहगाह हुआ करता था। संसद और साउथ ब्लाक व नोर्थ ब्लॉक (सत्ता केंद्र) के वाक् युद्धों ज़ी रपटें फाइल करने के बाद मैं भी कॉफी के प्याले में हठात् उठनेवाले तूफानों का मज़ा लेने पहुंच जाया करता था। लेकिन रहता मैं ‘आउटसाइडर` ही था।
कॉफी हाउस में सनातनी भाव से रमनेवाले ‘इनसाइडरों` में विष्णु प्रभाकर, रमाकांत, पंकज बिष्ट, राजकुमार सैनी, द्रोणवीर कोहली, केवल गोस्वामी, अरुण प्रकाश, डॉ. रमेश सक्सेना, आनन्द प्रकाश, रमेश उपाध्याय, चंचल, मस्तराम कपूर जैसे सूक्ष्म प्रज्ञा सम्पन्न सर्जनात्मक लेखक शुमार हुआ करते थे। वैसे शनिवार के ‘प्याले में तूफान` की रौनक कुछ अलहदा ही हुआ करती थी। हर शनिवार इनसाइडरों का दायरा फैला हुआ होता था, आउटसाइडरों और कैजुअल आप्रवासियों ज़ी आमद ख़ूब हुआ करती थी। गाइडेड मिसाइल की भांति दिल्ली बाहर के सर्जनकर्मी और बुद्धिजीवी मोहनसिंह प्लेस पर आ धमकते और तूफान के उतार-चढ़ाव में अपना योगदान भी दिया करते। तब मुल्क में राजीव का राज हुआ करता था, चारों ओर कंम्प्यूटर संस्कृति का जयघोष था और इक्कीसवीं सदी के पूंजीवाद के आगमन ज़ी शहनाइयां गूंजा करती थीं। क्या राजीव गांधी विकसित व उन्नत पूंजीवाद इस मध्ययुगीन भारत में ला सकेंगे?` जैसा सवाल हम सभी को बौद्धिक मुठभेडों के लिए उकसाया करता था। आग़ाज़ से पहले यह तयशुदा था कि ‘प्याले का तूफान` न थमेगा, न ‘डाईडाउन` होगा, और न ही किसी मंज़िल पर पहुंचेगा। बस! हम लोग यूं ही प्यालों के ईद-गिर्द भिनभिनाते हुए अपने-अपने ग़र्दो-ग़ुबार के तूफान की शक्ल़ देते रहेंगे। किफायती बिल चुकाते हुए ख़रामा-ख़रामा सीढ़ियों से उतर जाएंगे और बस स्टैंड ज़ी तरफ लपकने लगेंगे। हममें से कई ‘भगोडे` थे (मुझ समेत) जो संकल्प व उत्सर्ग की पांतों से चुपचाप व शातिरी से निकल आये थे। ‘एस्टेब्लिशमेंट` के कल-पुर्जे बन चुके थे। पर पांतों के तोडने या भागने के अपराध (या पाप) बोध से ग्रस्त ज़रूर हम रहते थे। यह बोध, यह हैंगओवर ही थे जो ‘प्याले का तूफान` का सूत्रपात किया करते थे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसे मर जाने के लिए छड देते थे। अगली शाम फिर नये अंदाज में उठने के लिए।
उन दिनों सैनी से काफी घुटा करती थी। वैसे पंकज बिष्ट और इब्बार रब्बी मेरी खिड़की हुआ करते थे, साहित्य की दुनिया की। इन दोनों के माध्यम से मैं इस दुनिया में ताक-झांक कर लिया करता था। लेकिन सैनी के साथ भी चर्चाएं कम नहीं हुआ करती थीं। कॉफी हाउस के बाद हम दोनों प्रेस- क्लब पहुंच जाया करते थे और ‘मय` में से नया तूफान पैदा किया करते थे। ज़्भी-ज़्भी सैनी के घर या मेरे यहां तूफान उठा करते थे। घरेलू प्यालों में। मैं उन दिनों जंगपुरा एक्टेंशन में रहा करता था। तब मेरे पास फीएट कार हुआ करती थी। क़ॉफी हाउस की सत्र-समाप्ति के पश्चात हम दोनों इस पर सवार हो लिया करते थे।
एक रोज! राजकुमार सैनी ने प्रस्ताव रखा कि मेरे यहां ‘पोस्ट कॉफी हाउस महफिल` लगे। सैनी चाहते थे कि इसमें अरुण प्रकाश को भी शामिल किया जाए। उन दिनों अरुण, मालवीय नगर रहा करते थे, और सैनी, आर. के. पुरम बस्ती में। इस प्रस्ताव को लेकर मैं दुविधा में पड़ गया। क्योंकि अरुण के प्रति अजीब किस्म के भाव मेरे मन में रहा करते थे- संकोची, निरीह, कुंठाग्रस्त, औसत बौद्धिक कद, अन्तर्मुखी और पूरी देह पर ‘रस्टिकपन` मले हुए। लम्बा-खुरदुरा चेहरा, चीखट बाल, ऊबड़-खाबड़ दाड़ी, मोटे-मोटे लम्बे-लम्बे दांत, कंजूसी भरी या रुंधी हंसी, बेतरतीब कमीज-पैंट, चप्पल-जूते वग़ैरह वगैरह। ‘वेरी अनइम्प्रेसिव करेक्टर` मेरे लिए अरुण प्रकाश थे। किसी तरह की तब ‘धाक` उनकी जमी हुई नहीं थी। स्पष्ट शब्दों में, मैं अरुण को अपने घर ले जाने के लिए कतई उत्साही नहीं था तब तक क्योंकी मेरी स्कीम में अरुण के लिए बिलकुल जगह नहीं बनी हुई थी।
मैंने सैनी को निरुत्साहित किया। हालांकि सैनी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा भी था कि अरुण एक होनहार कहानीकार है। प्रतिबद्ध लेखक है। कामरेड है। इसे साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं, सैनी और अरुण की
घनिष्ठता से परिचित था। दोनों के पारिवारिक रिश्ते थे। पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और सैनी का प्रस्ताव यह कह कर टाल दिया कि अगली बार देखेंगे। फिलहाल हम दोनों ही जाम से जाम टकराते हैं। आज की शाम, हम दोनों के नाम। सैनी ने मेरा इरादा भांप लिया। अपना प्रस्ताव ‘फिर कभी` के लिए मुल्तवी रखा। बहरहाल, उस रोज मैंने अरुण को भी कार में लिफ्ट दे दी, और डिफेंस कॉलोनी फ्लाइओवर के बस स्टाप पर छोड दिया। मैं और सैनी, जंगपुरा एक्सटेंशन की दिशा में मुड गये। जब जब प्याले टकराये, सैनी को अरुण की याद आती रही। शायद, मैंने भी दिल के किसी कोने में अरुण ज़ी नामौजूदगी का मलाल महसूस किया। इस तरह, एक अदृश्य अनमनेपन के साथ अरुण के प्रति मेरी दिलचस्पी का सिलसिला शुरू हुआ।
अरुण प्रज़श के प्रति उदासीनता की वजह थी। मैंने तब तक उनकी एक भी रचना पढ़ी नहीं थी। सिर्फ सुना ही करता था कि अरुण मूलत: कहानीकार हैं। बिहार के हैं। बहुत खुद्दार किस्म के जीव हैं। वे न आसानी से खुलते हैं, और न ही किसी को अपने निजीपन में झांकने देते हैं। अरुण ईगोइस्ट हैं, और जटिल भी। कभी-कभी यह भी सुनने को मिला कि अरुण का ‘सिमटापन` या ‘अन्तर्मुखिता` (विद् ड्रॉन) एक प्रकार का ‘आत्म-कवच` या ‘डिफेंस मैकेनिज्म़` है। क्योंकि अरुण हमेशा ‘अस्मिता संकट` से ग्रस्त रहते हैं। यह महानगर उसे लील न ले, इस भय का प्रेत अरुण के पीछे हमेशा दौडता रहता है। अरुण के लिए दिल्ली अजनबी थी, यह बात नहीं थी। वे इससे छठे दशक से परिचित थे। अरुण के पिता तब राज्यसभा के सदस्य बने थे। समाजवादी पृष्ठ भूमि से थे। सांसदों की बस्तियों में से एक, नॉर्थ ब्लाक में रहते हुए अरुण ने अपने पिता के साथ इस सत्ता नगरी के तेवरों-नखरों की नाप-तौल शुरू की थी। इसके ठोसपन और पोलेपन, दोनों से अरुण वाकिफ थे। मुझे याद है, कई वर्ष बाद जब हम दोनों के बीच घनिष्ठता हुई तब वे बताया करते थे कि उनके यहां कैसे-कैसे नेताओं की आवाजाही लगी रहती थी। इनमें से दो व्यक्तियों का विशेष रूप से ज़िक्र आया करता था- ललितनारायण मिश्र और फील्ड मार्शल मानेक शाह! वैसे समाजवादी नेता तो आया ही करते थे। अरुण ने इस ‘रूलिंग ईलीट` को ग़ौर से देखते हुए अपने दृष्टि -व्यिक्तत्व को तैयार किया था।
मित्रता के लम्बे अरसे के बाद अरुण प्रकाश ने स्वीज़र किया था कि ‘मैं ईगोइस्ट हूं, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका अस्तित्व ही शो-ऑफ पर टिका हुआ है।` दरअसल, बिहार के बेगूसराय जिला के निपनिया गांव से निकला यह तरुण इस महानगरी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की ललक से निरंतर लबरेज़ रहा है। एक दिन अरुण ने मुझे बताया था- ‘भाई जोशीजी! मैं सांसद का बेटा था। नॉर्थ ब्लाज़् में मैं साईकिल पर सवारी किया करता था। शर्ट की कॉलर ऊंची रखा करता था। मामूली जूते पहना करता था, अकसर चप्पलें। मेरी इच्छा रहती थी किलोग यह महसूस करें कि- देखो एम.पी. का बेटा साईकिल चला रहा है। वे मुझ पर गर्व करें.` मैं यहां साफ कर दूं कि अरुण ने मुझे इसकी कभी जानकारी नहीं दी थी कि उसके पिता सांसद थे।
जहां तक मुझे याद है, राजकुमार सैनी ने ही अरुण के पिता के संबंध में बतलाया था। वैसे मैंने संसद ज़ी रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, और मेरी ‘बीट` भी राज्यसभा थी। अरुण के मन में दो बातें रही होंगी- एक, अरुण अपने राजनीतिज्ञ पिता की छाया से स्वतंत्र होकर अपनी छवि-सत्ता बनाए। दो, अरुण के यार-दोस्त यह ज़रूर जानें कि उसके पिता सांसद हैं या थे लेकिन वे अपने ढंग से जानें। अरुण स्वयं इस जानकारी का माध्यम नहीं बनना पसंद करते थे।
राजस्थान के किसी राजे-रजवाड़े के म्यूज़ियम में एक बड़ी पेटी देखी थी। उस पेटी में अनेक पेटियां समाई हुई थीं। एक पेटी में से दूसरी पेटी निकलती, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी, और इस तरह से यह सिलसिला करीब दर्जन भर पेटियों तक चलता रहता। अंतिम पेटी में एक ख़ूबसूरत, चमकदार हीरा नमूदार होता। अरुण प्रकाश की बाहरी काया से भीतरी काया तक की यात्रा कुछ इसी किस्म की है। अरुण ने अपने व्यवहार, दृष्टि और क्रम शैली को काफी जतन से तराशा है। वे स्वयं के ‘अहर्निश चौकीदार` हैं। इस संबंध में एक घटना याद आती है।
पिता के असामयिक निधन के पश्चात अरुण प्रकाश की नये सिरे से संघर्ष यात्रा शुरू होती है। सत्ताधीशों की बस्ती से वे उजड़ जाते हैं। जीवनयापन के लिए अरुण ‘वेटर` बन जाते हैं, लोधी होटल में। एक रोज अरुण का सामना अज्ञेयजी से होता है। वे इला डालमिया के साथ डिनर के लिए वहां पहुंचे हुए थे। अरुण एक प्रोफेशनल वेटर के रूप में दोनों को डिनर ‘सर्व` करते हैं। अज्ञेयजी वेटर से हाल-चाल पूछते हैं। बिल सामने रखा जाता है और इला उसे अदा करती हैं, और साथ में ‘बख्श़ीश` भी देने लगती हैं। लेकिन अज्ञेयजी उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। इला बख्श़ीश राशि को अपने पर्स के हवाले कर देती है। अज्ञेयजी अरुण की ओर देखते हैं, और फिर इला की ओर। अरुण से हाथ मिलाकर अज्ञेयजी रेस्तरां से बाहर निकल जाते हैं। और उनके साथ-साथ इला डालमिया। अरुण अकेले ‘फ्रेम` में रह जाते हैं, आलोकित चेहरा लिए। बीती सदी के अंतिम दशक की शुरुआत में अरुण ने यह घटना सुनायी थी। ‘अज्ञेयजी बहुत ही संवेदनशील व्यिक्त थे। वे मेरे आत्म-स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इलाजी को बख्श़ीश नहीं देने दी। वे मुझे जानते थे। पिताजी को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने स्नेह से पूछा था – ‘कहो कैसे हो? यदि कोई काम हो तो नि:संकोच बतलाना।` मैंने कहा था ‘जी, अवश्य।` उन्हें प्रणाम किया, और चले गये।` अरुण ने जिन स्मृतियों को मेमने की तरह रखा हुआ है, उनमें से यह एक थी। सचाई यह है कि अरुण ने अपने पिता के किसी भी दोस्त का ‘ऑब्लीगेशन` लेना पसंद नहीं किया। कबीना मंत्री ललितनारायण मिश्र और अंकल सैम (मानक शाह) का भी नहीं।
कष्टों को निमंत्रण देने की ‘एक्सपर्टीज` अरुण प्रकाश ने अर्जित कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे कहानी लेखन में। अरुण के पात्रों ज़ी भांति अरुण के कष्टों की भी रचना की जाती है। अरुण ने अपने बल-बूते पर कष्टों को झेला और चलताऊ नौकरियां कीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक निगम के जन-सम्पर्क विभाग में हिन्दी अधिकारी के पद पर भी रहे। यह बिल्कुल स्थायी व सुरक्षित नौकरी थी। लेकिन मेरे यार को यह मंजूर नहीं था कि वह सुरक्षा व सुविधाओं को चिपकाए फिरे। एक दिन मेरे केबिन में आकर घोषणा की- ‘भाई साहब! मैंने नौकरी छोड दी है।` मैं यह सुनकर अवाक रह गया। ‘अब क्या प्लान है?` मैंने पूछा। ‘सक्रिय पत्रज़रिता में कूद पड़ा हूं। जागरण का दिल्ली संस्करण निकल रहा है। संपादक कमलेश्वरजी होंगे। मैं सहायक संपादक हूंगा।` मुझे यह कदम अजीब सा लगा। राजकुमार सैनी भी इससे सहमत नहीं थे। कॉफी हाउस के इनसाइडर और आउटसाइडर दोस्तों ने भी इस निर्णय का स्वागत नहीं किया। इसके दो कारण थे- एक जागरण मुख्यत: भाजपाई अख़बार था। दो, कमलेश्वरजी लम्बे समय तक संपादक बने रहेंगे, इसमें सभी को संदेह था। और यही हुआ भी। कमलेश्वरजी जागरण से चलते बने, और अरुण फिर सड़क पर थे। नई नौकरी की तलाश शुरू हो गई।
कई दिनों के बाद मैंने अरुण से पूछा कि अब आगे की योजना क्या है? ‘मैं पत्रकारिता में डटा रहूंगा। फ्रीलांसिंग करूंगा। मैंने अपनी ज़मा पूंजी का हिसाब-किताब कर लिया है। दिलशाद गार्डन में एल.आई.जी. मकान ले लिया है। एक कमरा और एक छोटा सा ड्राइंग रूम है। और साथ में एक बॉलकनी, जो कि व्यंग्य थी। इसमें कथाज़र अरुण ने अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया। चार अदद लोगों का परिवार। और इसी जगह से आरम्भ होती है बड़ी रचनाओं की रचनायात्रा।
अरुण की फितरत नहीं है कि उसे ‘पराजित सैनिज़्` के रूप में जाना जाए। उसकी यही फितरत उसके पात्रों में बार-बार गूंजती है। एक ऐसी गूंज जो खामोशी के साथ उठती है, खामोशी से गूंजती है, और खामोशी के साथ पूरे माहौल पर बिखर जाती है। इस गूंज में कहीं प्रदर्शन नहीं है, न ही चीख़, न ही विजय व उत्सर्ग की उद् घोषणाएं और न ही नारे। लेकिन एक हैरतभरी विस्फोटकता इस खामोशी भरी गूंज में समाई हुई रहती। और शायद यही है मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य की अस्मिता का जयघोष। सुन्दरी मामी (कहानी-ना) सुश्री एक्का (बेला एक्का लौट रही है), कम्मो (विषम राग) मस्तान (गज पुराण) जैसे अनेक पात्रों में ये ही गूंजें सुनाई देती हैं।
तभी एक रोज़ मालूम हुआ अरुण प्रकाश राष्ट्रीय सहारा में जा पहुंचे हैं। हम सभी को आश्चर्य हुआ। दिल्ली की फुटपाथें अरुण के पांवों को लम्बे समय तक कैसे बांधे रख सकती थीं? अरुण, जागरण से छूटे, राष्ट्रीय सहारा में पहुंचे। जहां तक मुझे याद है, यह समय का था। एक अल्ल-सुबह अरुण मेरे घर आ धमके। मैं घबराया। ‘ क्या माजरा हो सकता है ?` स्वयं से सवाल किया। सोचा, कोई फिर नई मुसीबत पैदा हो गई है। हो-न-हो, इसने राष्ट्रीय सहारा भी छोड दिया है। दिमाग कई प्रकार ज़ी आशंकाओं से घिर गया। खैर! अब क्या हो सकता है। जो भी होगा, फेस करेंगे। मैंने अपने भावों को छुपाए रखा। मधु (पत्नी) ने इसी बीच चाय तैयार कर दी। हम इधर-उधर की गपशप लड़ाते रहे। अरुण की एक फितरत यह भी है कि वे सामने वाले की गहरी थाह लेने के बाद ही अपने पत्ते खोलते हैं। बात खोलने के लिए वे जटिल प्रक्रिया से गुज़रते हैं। इसके विपरीत मेरी अधीरता है जो कि फूट पड़ती है। पत्रकार हूं, इसलिए तुरत-फुरत मुद्दे पर आ जाना चाहता हूं और सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू कर देता हूं। मुझे कोफ्त़ होने लगती है जब मुद्दे का प्लॉट तैयार करने में वक्त़ बर्बाद किया जाता है। ख़ैर! चाय आई, चाय ली और अरुण ने अत्यंत सावधानी के साथ मेरे सामने प्रस्ताव रखा- ‘भाई साहब! अब ‘नई दुनिया` से मुक्ति लीजिए। सहारा में आइए। पद और पैसा, दोनों मिलेगा।` यह सुनकर मैं चौंका। मैं तब तक ‘नई दुनिया` में ग्यारह-बारह वर्ष ज़ी सर्विस कर चुका था। दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख के रूप में। आधी दुनिया देख डाली थी, देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों के राजकीय दौरों के कवरेज के सिलसिले में। ‘मुझे इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए समय दो।` मैंने अरुण को टाल दिया। लेकिन अरुण हार मानने वाले जीव नहीं थे। तीन-चार रोज की कवायद के बाद मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे मुझे राष्ट्रीय सहारा के कर्ताधर्ता सुब्रतो राय से मिलाने के लिए ले गये। उनके साथ तीन-चार मीटिंगे हुईं। इन मुलाकातों में वेतन से अधिक वैचारिक मुद्दे अधिक छाये रहे। अरुण ने राय साहब को मेरी साम्यवादी पृष्ठ भूमि के बारे में पुख्त़ा ढंग से पहले से ही समझा दिया था। और अन्तत: मैं भी सहारा पहुंच गया। इस घटना ने कॉफी हाउस के दोस्तों को हिला कर रख दिया। अरुण को ज़फी भला-बुरा कहा गया, और मुझे भी। मेरे एम. ए. के सहपाठी पंकज बिष्ट सबसे अधिक खफ़ा थे। वे इस ह़क में नहीं थे कि मैं नई दुनिया छोडकर सहारा को ज्वाइन करूं। राजधानी के पत्रज़र बंधुओं ने भी मेरे इस कदम को नापसंद किया। क्योंकि मित्र मंडली मेरे और सहारा के मिज़ाज से पूर तरह परिचित थी। दोनों के बीच लम्बे समय तक निभेगी, इसे लेकर सभी को गहरी शंका थी। ख़ैर! जीवन में प्रयोग होते रहने चाहिए। मित्रों की भविष्यवाणी सही निकली। मैंने ड़ेढ महीने काम किया, और फैक्स से इस्तीफा भेजकर वापस नई दुनिया में अपने पूर्व मोर्चे को सम्हाल लिया। लेकिन यहां यह साफ कर दूं, मेरे छोडने से चौबीस घंटे पहले अरुण भी राष्ट्रीय सहारा को अलविदा कह चुके थे। वे फिर से फुटपाथ पर थे। कॉफी हाउस के इनसाइडरों से घिरे हुए थे। मैं संसद का मानसून सत्र कवर कर रहा था। दोनों ने तय करके इस्तीफे नहीं दिये थे। बल्क दोनों ने एक दूसरे को अपने इस्तीफे के इरादे और भेजने के समय की भनक तक नहीं लगने दी। मेरे इस्तीफे की क्या पृष्ठ भूमि थी, इसकी अलग कहानी है। वह फिर कभी कही जाएगी। फिलहाल, यहां इतना कहना काफी होगा कि अरुण प्रकाश ने पुन: ‘आत्मपीड़न` को लम्बी दावत के लिए आमंत्रित कर डाला था। अरुण एक ‘टिपीज़्ल मैसोकिस्ट` हैं। त़क़रीबन दस बरसों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तब से ही।
मैंने शुरू में स्वीकार किया था कि मैंने लम्बे समय तक अरुण प्रकोश को तरजीह नहीं दी थी। वे मुझसे मिलते, कभी कॉफी हाउस, कभी मेरे ब्यूरो (आई.एन.एस. स्थित) में। चलताऊ किस्म ज़ी मुलाकातें होती रहीं। कोई अनोखापन उनमें मुझे नज़र नहीं आया। वास्तव में अरुण रिश्तों ज़ी कैमिस्ट्री सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं। बीरबल की खिचड़ी की तरह संबंधों को पकाते रहते हैं। जल्दबाज़ी, उनके लिए अजनबी शब्द है । अरुण को ‘लिफ्ट` नहीं देने ज़ी वजह यह भी रही कि मैंने तब तक उनज़ी कोई रचना नहीं पढ़ी थी। यद्यपि, तब तक कई कहानियां पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुज़ी थीं। में अरुण की दो पुस्तकें : कोंपल कथा (लघु उपन्यास) और जल प्रांतर (कहानी संग्रह) देखने को मिलीं। मुझे यह स्वीकोर ज़्रने में कतई हिचक नहीं है कि ‘कोंपल कथा` से कहीं अधिक उनकी कहानियों ने प्रभावित किया था। यद्यपि मैं साहित्य की किसी भी विधा का आधिकारिक पारखी नहीं हूं। अंग्रेजी साहित्य में एम.ए करने के बावजूद, मेरा मन-मस्तिष्क साहित्येतर विषयों (समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र आदि) में ही ज्य़ादा रमता रहा है। चूंकि इब्बार रब्बी, पंकज बिष्ट जैसे सहपाठी रहे हैं तो साहित्य के साथ भी मैं जब-तब ‘फ्लर्ट` करता रहा हूं। सो ‘जल-प्रांतर` में जमा छह कहानियों में से ‘जल-प्रांतर` मुझे प्रत्येक दृष्टि से अद्वितीय लगी। एक जबर्दस्त कहानी। अरुण ने इसमें अपना सब-कुछ उलीच कर रख दिया। मनुष्य, ज़ल और व्यवस्था का एक यथार्थवादी रूपक कहानी का नायक पंडित वासुदेव का किरदार एक साथ कई द्वंद्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ‘जल-प्रांतर` सिर्फ बाढ़ से घिरे लोगों और इलाके की कानी नहीं है। मैं इसे राष्ट्र के संधिज़ल के अन्तर्विरोधों के रूपज़् के तौर पर लेता हूं।
अरुण प्रकाश से आत्मीयता की शुरुआत हुई… सिलसिला बढ़ता चला गया। यह आज तक बदस्तूर है। एक दिन शाम मेरे यहां अरुण आ धमके। मेरे हाथों में एक किताब थमा दी। किताब की सूरत-मूरत देखकर लग रहा था, यह अभी-अभी जन्मी है। बाइंडर या प्रज़शक के यहां से इसकी डिलवरी लेकर जनाब थामे चले आ रहे हैं। पुस्तक ज़ टाइटिल था- ‘लाखों के बोल सहे`। ‘इसे खोल कर देख लीजिए जोशीजी।` अरुण बोले। मैंने पुस्तक खोली, और स्वयं को आत्मीयता के गर्भगृह में पाया। यह कहानी संग्रह मुझे समर्पित था- ‘मेरे अनन्य रामशरण जोशी जिन्होंने लाखों के बोल सहे।` हृदय में बसंत फूटा। मैं कृतज्ञ हुआ। पर इसे व्यक्त करना, आत्मीयता को औपचारिकता के सांचे में पिघलाना होगा। ख़ैर! ग़ालिब के अंदाज़ में शाम गुज़री… इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा ‘ग़ालिब छुटी शराब (बकौल कालियाजी)`।
एक शाम। घर पर कुछ आदरणीय- नामवरजी, राजेन्द्र यादव, केदारजी, विश्वनाथ त्रिपाठीजी, शर्माजी, विजय मोहन सिंहजी और मित्रों में थे- इब्बार रब्बी, अरुण प्रकाश, रमेश सक्सेना, कुलदीप आदि जमा हुए। शायद कोई पुरस्ज़र मिला था। तो कुछ तो होना ही था। सो हुआ- और ‘चलताऊ कॉकटेल` चल पड़ी। तब अरुण का नया रूप भी सामने आया और वह था अपने वरिष्ठों के साथ किस प्रकार ‘समानता और सम्मानता` की धार पर चलते हुए व्यवहार किया जाता है। वरिष्ठों ने उन्हें ग़ौर से सुना, ग़ौर से समझा। तब लगा, अरुण को कैज़ुअल तरीके से ‘डिसमिस` नहीं किया जा सकता। देर-सबेर इसमें ‘दम` है यह स्वीकार करना होगा।
अरुण प्रकाश एक ऐसा शख्स है जिस पर खुद से अधिक भरोसा किया जा सकता है। बग़ैर किसी प्रदर्शन के वह आप में उतरता चला जाएगा। इसको आपज़े पता भी नहीं चलेगा। ऐसा महसूस मुझे धीरे-धीरे हुआ। अरुण ज़ी रचनाएं पढ़ने के पश्चात लगा, इस व्यिक्त में टिकाऊपन और खरापन, दोनों ही हैं। अरुण के चरित्र ज़ी बड़ी खासियत यह भी है कि ‘जड़ों की सोंध` उसमें हरदम महकती रहती है। ‘कोंपल कथा` से लेकर ‘विषम राग` तक की रचनायात्रा में अरुण के संग-संग चलने वाले सभी पात्र अपनी जड़ों से गहराई तक जुडे हुए हैं। वे छिटकते भी हैं तो वापस उन्हीं तक पहुंच जाते हैं। बनावटी एलिएनेशन से वे बिल्कुल मुफ्त हैं। पात्रों का भौगोलिक और भावनात्मक फैलाव होता भी है तो जड़ें उनके लिए कुतुबनुमा का रोल अदा करती हैं। ‘भैया एक्सप्रेस`, ‘मंझधार किनारे`, ‘विषम राग`, ‘गज पुराण`, ‘तुम्हारा सपना नहीं`, ‘कहानी नहीं` जैसी रचनाओं में जड़ों की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। कभी कभी या अकस़र मुझे लगता है, अरुण प्रकाश के पात्र उनके विभिन्न चारित्रिक आयामों के विस्तार हैं। और यही बात अरुण में भरोसा पैदा करने के लिए मुझे बाध्य करती है।
अब देखिए। अरुण प्रकाश को इस महानगर में रहते हुए दो दशक से अधिक समय बीत चुका है। करीब सोलह-सत्रह सालों से हम एक-दूसरे को जानते हैं। एक-दूसरे के यहां आते-जाते भी हैं। इस क्रम में न कोई औपचारिकता होती है, न ही कोई पूर्व सूचना। हम दोनों का एज़् कॉमन दोस्त हैं- अरविंद जैन। स्त्री मामलों के विशेषज्ञ और राजेन्द्र यादवजी अर्थात् हंस के संपादज़् के भूतपूर्व कानूनी सलाहकार। अरविंद का चैम्बर चौथे माले पर खुले आसमान में लालटेन की भांति टंगा रहता है। मैं इसे अरविंद ज़ी अटारी या अटरिया बोलता हूं। यहीं शाम ज़ी बैठकें होती हैं। इस अटरिया की शामों में वे ही लोग शामिल होते हैं जो कॉफी हाउस जाने से परहेज करते हैं। पिछले कुछ सालों से सैनी ने भी जाना बंद कर दिया है। इसके कई ज़रण हैं जिनका यहां ज़िक्र ज़रूरी नहीं है। बस! यहां इतना जान लेना पर्याप्त है कि अरुण के बग़ैर अटरिया की शाम फीकी रहती। अरुण को इसज़ कभी गुमान नहीं होता है कि वे लेखक हैं। उन्हें सिर्फ यह याद रहता है कि वे इंसान हैं। इसके आगे या पीछे विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक लेखज़् के तौर पर तवज्जोह मिल रही है या नहीं, अटरिया की शाम या किसी और की महफिल में, इसकी चिंता अरुण को नहीं है। अरुण सलीके से बड़ी महीन मार के साथ अपनी बात रखते हैं, और चेहरों को पढ़ते हुए लम्बी चुप्पी साध लेते हैं।
मुझे याद है। दिल्ली के साहित्यिक गलियारों में नब्बे के दशज़् के मध्य तक अरुण प्रकाश को उनज़ ‘ड्यू` मिलना शुरू नहीं हुआ था। यद्यपि, तब तक उनज़ी पांच-छह पुस्तकें आ चुकी थीं। इनमें ‘लाखों के बोल सहे` जैसी चर्चित कहानी संकलन भी शामिल है। तब एक ‘रिज़र्वेशन` अरुण लेकर बना रहता था। कितपय कथाकार-पत्रकार-संपादक उन्हें ‘कहानीज़र` मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक-दो की टिप्पणियां आज भी मुझे याद हैं। मसलन, एक कवि-कम-कहानीकार ने फ़ब्ती कसी- ‘ क्या जोशीजी अरुण प्रकाश को साथ लगाये रखते हो। वो कहां का कहानीज़र हुआ?` एक दूसरी टिप्पणी में उन्हें ‘बिहार की खोल` कहा गया क्योंकि उनकी कहानियां बिहार की सरहदों से बाहर झांकती ही नहीं हैं। ‘अरुण की कहानियां सीधी-सपाट हैं। न उनके कथ्य में द्वंद्व है, न क्राफ्ट, न भाषा, न शैली। समाज ज़ी जटिलताएं बिलकुल ग़ायब हैं।` जैसी टिप्पणियां उन पर चस्पां कर दी जाती थीं। संक्षेप में अरुण को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता था। महानगर के ‘साहित्यिक रूलिंग ईलीट` में उदय प्रकाश, स्वयं प्राश जैसे समकालीनों के नाम उछला करते थे। अरुण का नाम कहीं अंतिम कतार में ज़रूर सुनाई दे जाता था। लेकिन, मैंने देखा मेरे यार ने अपना सफर जारी रखा और सुरंग बनाता रहा। ‘रूलिंग ईलीट` ने सोचा ‘बेचारा अरुण फ्रीलांसिंग कर रहा है। अनुवाद और विज्ञापन कॉपियां इधर-उधर लिख कर कमा खा रहा है। चिंता की बात नहीं है। मैंने महसूस किया, अरुण को लेकर ‘हमदर्दी` के भाव ईलीट सर्कल में रहा करते थे। एक दिलचस्प टिप्पणी मुझे आज भी याद है। किसी हैसियतमंद लेखक के साथ गपशप चल रही थी। अरुण का ज़िक्र अचानक फुदक पड़ा। फिकरा फूटा, बेचारा कमलेश्वर दंश का सताया हुआ है। अच्छी-भली सरकारी नौकरी की। कमलेश्वर के चक्कर में फंसकर अपनी चाल भी भूल गया। इस इम्प्रेशन ने अरुण को ईलीटों की ‘अलाय-बलाय` से बचाए भी रखा। और उन्हें सुरंग बिछाने ज़ मौका मिल गया।
कुछ देर पहले मैंने ज़्हा था, अरुण प्राश अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद इंसान हैं। इसकी कई वजह हैं। और ये सभी निजी अनुभवों पर टिकी हुई हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो गर्दिश में भी मल्हार गाएं, और पतझर में बसते हुए बसंत ज़ी अनुभूति से आपको समृद्ध करें। अरुण को ऐसे लोगों में बेखटके रखा जा सकता है। बीते दशक में, मैंने उन्हें कुछ ‘एसाईन्मेंट` सौंपे थे। पारिश्रमिक ज़ी चिंता से पहले अरुण की परेशानी यह हुआ करती थी कि काम परफेक्शन के साथ हुआ या नहीं। संभव है, कई दफे उन्हें उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ। लेकन, संबंधों को प्राथमिकता दी गई। कई चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यों को निश्चित अवधि में निपटाया। इसकी अलग कहानी है। अरुण का स्वास्थ्य अरुण की इच्छाशक्ति का बंधक रहता है। आश्चर्यजनक ढंग से। अरुण भी इसके साथ नाना प्रयोग करते रहते हैं, कभी प्राकृतिक चिकित्सा, कभी ऐलोपेथी, कभी होमियोपेथी, और कभी ‘बेदर्दी-थेरेपी`। पर मजाल है, किसी का कामम रुक जाए। पिछले दिनों मुझे अपने विश्वविद्यालय (भोपाल स्थित) के प्रसारण पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए पटकथा लेखन पर कार्यशाला की ज़रूरत हुई। अरुण से इसका ज़िक्र किया। अस्वस्थता के बावजूद वे कडाके की सर्दी में भोपाल एक्सप्रेस से रवाना हो गए। सप्ताह भर धुंआधार कार्यशाला लगाई और विद्यार्थी उन पर फिदा। यह एक नहीं, ऐसे कई अनुभव हैं।
वास्तव में, हम हिंदी के लोग ‘प्रोफेशनलिज्म़` के नाम से चिढ़ते हैं। इसे मिशन का बैरी मानते हैं। यदि हम प्रोफेशनल बन गये तो हमारी आत्मिक व नैतिक शुचिता भंग हो जाएगी। प्रोफेशनल बनने का अर्थ है स्वेच्छा से अपना शीलहरण करवाना। हिंदी पत्रकारिता में पिछले लम्बे समय से आत्म रोदनका दौर चल रहा है। वजह है ‘हाय! अब हम गणेशशंकर विद्यार्थी क्यों न रहे?` कोई यह नहीं कहता कि ‘प्रोफेशनल` यों नहीं बनते? कतिपय ‘पत्रकार महंत` लाला से खासी ‘पगार और पर्क्स` वसूलते हैं, और फ़िदायीन अदा में ‘मिशन हरण` के लिए स्यापा भी करते हैं। हिंदी के रूलिंग ईलीटों की हालत भी इससे भिन्न नहीं है। वे आत्मविलाप व आत्मदीनता में धंसे रहते हैं। इस जमात के कुछ सदस्य दूसरे-तीसरे साल अपना वाहन बदल डालते हैं लेकिन अरुण प्रकाश के चेहरे पर चमक दिखाई दे, यह उन्हें मंजूर नहीं है। अरुण ने प्रोफेशनलिज्म़ के मिशन के रूप में लिया है। यह कबीर का वक्त़ नहीं है। यह युग है विक्रम सेठ, सलमान रश्दी, शोभा डे जैसों का, जिन्हें लिखने के लिए मोटी रकम अग्रिम दी जाती है। मैं मिशन, प्रोफेशनलिज्म़ और ‘कॉमर्शियलाइज़ेशन` में फ़रक करता हूं। मैं समझता हूं अरुण भी इन तीनों में अंतर करते हैं। उनका प्रोफेशनलिज्म़, आजीविज़-अर्जन के उत्तरदायित्वों से जुडा हुआ है जिसे वे पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं। यही वजह है कि वे घाटा सहकर भी अपना कमिटमेंट पूरा करने से बिदकते नहीं हैं। हिंदी में ‘प्रोफेशनल एप्रोच` की बेहद कमी खटकती है। यद्यपि पिछले कुछ समय से इसे दूर करने के गंभीर प्रयास शुरू हो गये हैं। अरुण ऐसे ही प्रयासों का मस्तूल थामे हुए हैं।
मुझे स्वयं अरुण से ईर्ष्या होती है। साधनहीनता के बावजूद वे अपना चुंबकीय व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अरुण का किसी गोष्ठी में व्याख्यान हो और उसक ऊष्मा देर तक महसूस न होती रहे। यही वजह है कि आज अरुण को आसानी से ‘ख़ारिज` नहीं किया जा सकता। वैचारिक व व्यवहारात्मक निरंतरता और ‘प्रोफेशनल इंटेग्रिटी`, इसी ताकत के बल पर इस महानगर की जमुनापारी बस्ती दिलशाद गार्डन में अरुण ने अपना शीराज़ा जमा रखा है। बिखरने से बेख़ौफ़। अरुण को महानगरीय ‘सोफिस्टीकेशन` से चिढ़ है। इसके तौर-तरीकों को वे परले सिरे से नापसंद करते हैं। ‘पॉलसन` मारना तो कल्पना से बाहर है। इसीलिए राजेन्द्र यादव, डॉ. नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी जैसे ठिकानेदारों की ग़िरफ्त से खुद को बचाए रखते हैं। फिर भी अपनी हस्ती का एहसास कराते हैं। पिछले दिनों ‘विषम राग` पर आयोजित जलेस की गोष्ठी इसकी गवाही देगी। फिर अरुण को ‘ऑपरेटर` क्यों होना चाहिए?
मैं यह समझता हूं कि अरुण प्रकोश बाज़ार के मिज़ाज और उसके सेंसैक्स को देख कर नहीं लिखते हैं। इसीलिए उनी रचनाएं ‘कमोडिटी` क शक्ल नहीं ले पाती हैं, और न ही उस रूप में बिक पाती हैं। उनज़ी कृतियां ‘पाठकों` के लिए हैं, न कि ‘ग्राहकों` या ‘उपभोक्ताओं` के लिए। हैं ऐसे कतिपय कथाकार जो हैरतअंगेज़ अंदाज़ में अपनी रचनाओं को परोसते हैं। बाज़ार में ‘क्राफ्ट`को बेचा जाता है जो कि प्राणहीन होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से ‘लॉबिंग` का सिलसिला जम कर चला हुआ है। रूलिंग ईलीट के मेम्बरान अपनी अभिजातवर्गीय कोठियों और रेस्तराओं में शराब पार्टियां आयोजित कर अपनी पुस्तकें उछलवाते हैं। गोष्ठियां प्रायोजित की जाती हैं और भांति-भांति के विमर्श खड़ा कर स्वयं को स्थापित करने के लिए ‘उड़ान-पट्टी` तैयार की जाती है। आश्चर्य और दु:ख का विषय यह है कि ‘कतिपय नामधारी` भी उड़ान पट्टी की भूमिका निभाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। और इसी से बाज़ार व ग्राहक तैयार किए जाते हैं। तब इस ‘प्रायोजन-चक्रवात` में अरुण प्रकाश सरीखे लेखक और उनका लेखन तना रहता है, तो इस दौर ज़ी इसे ऐतिहासिक उपलब्धि ही कहा जाएगा।
मैं नहीं जानता, मैं कहां तक सही हूं? पर मेरी दृष्टि से ‘विषम राग` और ‘गज पुराण` को पिछले आधे दशक की हिन्दी कहानियों में ‘माइल स्टोन` के रूप में दर्ज किया जा सकता है। ‘विषम राग` की नायिका कम्मो नि:संदेह अद्भुत पात्र है। इस किरदार के माध्यम से अरुण जहां एक ओर पांच हजार वर्ष की ज्ञात सभ्यता के घृणिततम व अमानवीय पेशा (मैला ढोना) की प्रतिनिधि कम्मो के आंतरिक व बाह्य सौन्दर्य को आसमान प्रदान करते हैं, वहीं अमरबेल की तरह फैलती एपार्टमेंट-संस्कृति के अन्तर्विरोधों को भी उघाड़ कर रख देते हैं। कम्मो और एपार्टमेंट रहवासियों के अन्तरसंबंधों का इससे बेहतर ट्रीटमेंट अन्यत्र मिलता नहीं है। दरअसल अरुण की कहानियां बगैर शोर-शराबे के औरत-विमर्श को भी जन्म देती हैं। और इस विमर्श में विचारधाराओं, लिंग समानता, स्त्री मुक्ति आदि के नगाड़े सुनाई नहीं देंगे। पर कहानी के आरम्भ से पटाक्षेप तक, औरत अपनी सम्पूर्ण ओजस्विता के साथ हर दृश्य में मौजूद मिलेगी। इस नाते कुछ पात्राएं गिनाई जा सकती हैं। कम्मो, नीलम, अनिता राव, सुन्दरी मामी, बेला एक्का, रंजो, सबितरी आदि। अरुण के यहां औरत के संघर्ष, साहस, उत्सर्ग, पीड़ा, दुष्टता जैसे किसी चरित्र-निर्धारक व्यवहार का ग्लैमरीकरण नहीं है। बल्कि, स्वाभाविकता का आवेग ज़रूर है जो कि अतिशयता को स्पर्श कतई नहीं करता है। साफ शब्दों में- सब कुछ ‘सबड्यूड` है। कायदे से है।
कभी कभी अरुण के पात्रों में मुझे भीष्म साहनी के पात्रों की झलक दिखाई देती है। पर अलग ठेठ देसी अंदाज में। भीष्मजी के समान अरुण के ज्यादातर पात्र मामूली पृष्ठ भूमि के हैं लेकिन असाधारणता के विस्फोट से लैस हैं। जैसे-जैसे पाठक के पग बढ़ते जाते हैं, असाधारणता की माइनिंग विस्फोट करती रहती है। अन्त के छोर पर पहुंच कर एहसास होता है- अरे! यह क्या हुआ? इसके लिए ‘तुम्हारा सपना नहीं`, ‘भैया एक्सप्रेस`, ‘मंझधार किनारे`, ‘आखिरी रात का दुख`, ‘कहानी नहीं` जैसी रचनाओं में उतरना काफी होगा। इसलिए बिहारी बाबू के विषम राग में भीषण राग की अनुगूंज निराले अंदाज में सुनाई दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोनों के कंसर्न और उन्हें समझने की दृष्टि में भी तो साम्यता है। तब ‘अदना से साधारण` में पात्रों के रूपांतरण में हैरत कैसी? बस! अंदाज़ेबयां अपना-अपना है; फिर चाहे भीष्मजी की ‘कुंतो` हो या अरुण की ‘कम्मो`। दोनों रचनाकारों की एकमात्र मामूली इच्छा और कोशिश यह है कि उनके ऐसे पात्र बेहतर गरिमाभरी ज़िंदगी के ह़कदार बनें। इसीलिए बेला एक्का, यह फैसला ‘नहीं, थंगम्मा! सहना मरना है।` वक्त़ और व्यवस्था को ज़वाब देने के लिए काफी है।
इधर अरुण प्रकाश ज़े लेकर कुछ नई चर्चाएं चल पड़ी हैं। चर्चाओं में कितना दम है यह कहना कठिन है। पर यार लोग पीछे से यह कहते हैं कि अरुण ‘आत्ममोह` का रोग लग गया है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे ‘नार्सिस्ज्म़` ज़्हा जाता है। मित्रों ज़ी शिकायत है कि आपसी बैठकों में अरुण अपनी ही रचनाओं पर घुमा-फिरा कर फोकस में रखने का प्रयास करते हैं। कभी कभी महीन ढंग से वे स्वयं को इम्पोज़ भी करना चाहते हैं। इसके लिए वे उपक्रम रचते रहते हैं। किसी ने बतलाया कि उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब हिंदी में कहानी के तीन प्रकाश हैं- उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश और अरुण प्रकाश। इस ‘त्रि-प्रकाशमूर्ति` के ईद-गिर्द ज़्हानी संसार घूमता है। अरुण ज़ी व्यवहार शैली में यह ताज़ा दोष बार-बार झलज़्ता है। इससे ‘ग्रोथ` रुक सकती है। इस दोष के शमन की आवश्यकता है। मित्रों का मत है।
मैं इस दोष ज़े अरुण प्रज़श के चरित्र के ‘स्थायी भाव` के रूप में नहीं देखता हूं। यह ऐसे इंसान की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे लम्बे समय तक ‘लाखों के बोल` सहने पड़े हों या हाशिये पर रखा गया हो। अभी हाल ही में एक ताज़ातरीन अनियतकालीन पत्रिका के ताज़ा ताज़ा बने संपादक ने उन्हें फोन किया और कहा कि सुना है इधर तुमने कुछ कहानियां लिखी हैं। ‘कभी मुझे सुनाओ` यानी सुनने के बाद कहानी की प्रकाशन-पात्रता तय की जाएगी। या यह ‘अपेक्षा` अरुण को आघात पहुंचाने के लिए काफी नहीं है? और यह मांग भी ऐसे व्यक्ति ने की है जो स्वयं साहित्य और पत्रज़रिता में ‘स्थान` के लिए तट पर खड़ा है। बरसों से। तमाम गर्जन के साथ। लेकिन अरुण इसका मोहताज़ नहीं है।
इस दोष को मैं जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसे (यदि है तो?) समझने की कोशिश ज़रूर कररहा हूं। मेरे और अरुण के संबंधों पर महीनों तक पाला छाया रहता है। फोन पर बात नहीं होती है। शायद ही हम गोष्ठियों में टकराते हों। वर्ष भर में एक-दो ही ऐसे अवसर आते हों जब हम एक साथ मंच पर हों। लेकिन जब मिलते हैं तो फुरसत से, और पाला ख़ुद-ब-ख़ुद काफ़ूर हो जाता है। दिक्कत यह है कि हममें से अधिकाश सामंती और औपनिवेशिक जहनीयत से आज़ाद नहीं हो सके हैं। यह हम सोच ही नहीं पाते कि हाशिए के लोग भी ‘धुरी` बन सते हैं? कभी। तब अरुण या ऐसा ही कोई और ‘आत्ममोही` दीखता है तो इसमें ग़लत क्या है? या साधन सम्पन्न या रूलिंग ईलीट इसके लिए ‘प्रायोजित गोष्ठियों व दावतों` का सहारा नहीं लेते हैं? यह भी एक किस्म की ‘आत्मरति` है, भले ही परोक्ष रूप से सही। ‘परोक्ष आत्मरति` में तो पाखण्डाचार होता है जबकि ‘प्रत्यक्ष आत्ममोह` के लिए जागरूक (?) भृतकों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वहां ‘आत्मीयजन` होते हैं।
फिर भी इस दोष से ख़बऱदार रहने का अर्थ है सर्जनात्मकता को विस्तार देना। दोष ग्रस्त रहने के मायने है विलगाव व जड़ता। मैं समझता हूं, इस नोट पर इम्प्रेशन की इति की जा सकती है : ‘अरुण प्रकाश, न ग़ाफ़िल इंसान है, और न ही मग़रूर रचनाकार। समय की प्रवृत्तियों, व्यवस्था के चरित्र और मनुष्य की संवेदना के एक सिंसीयर पारखी है।